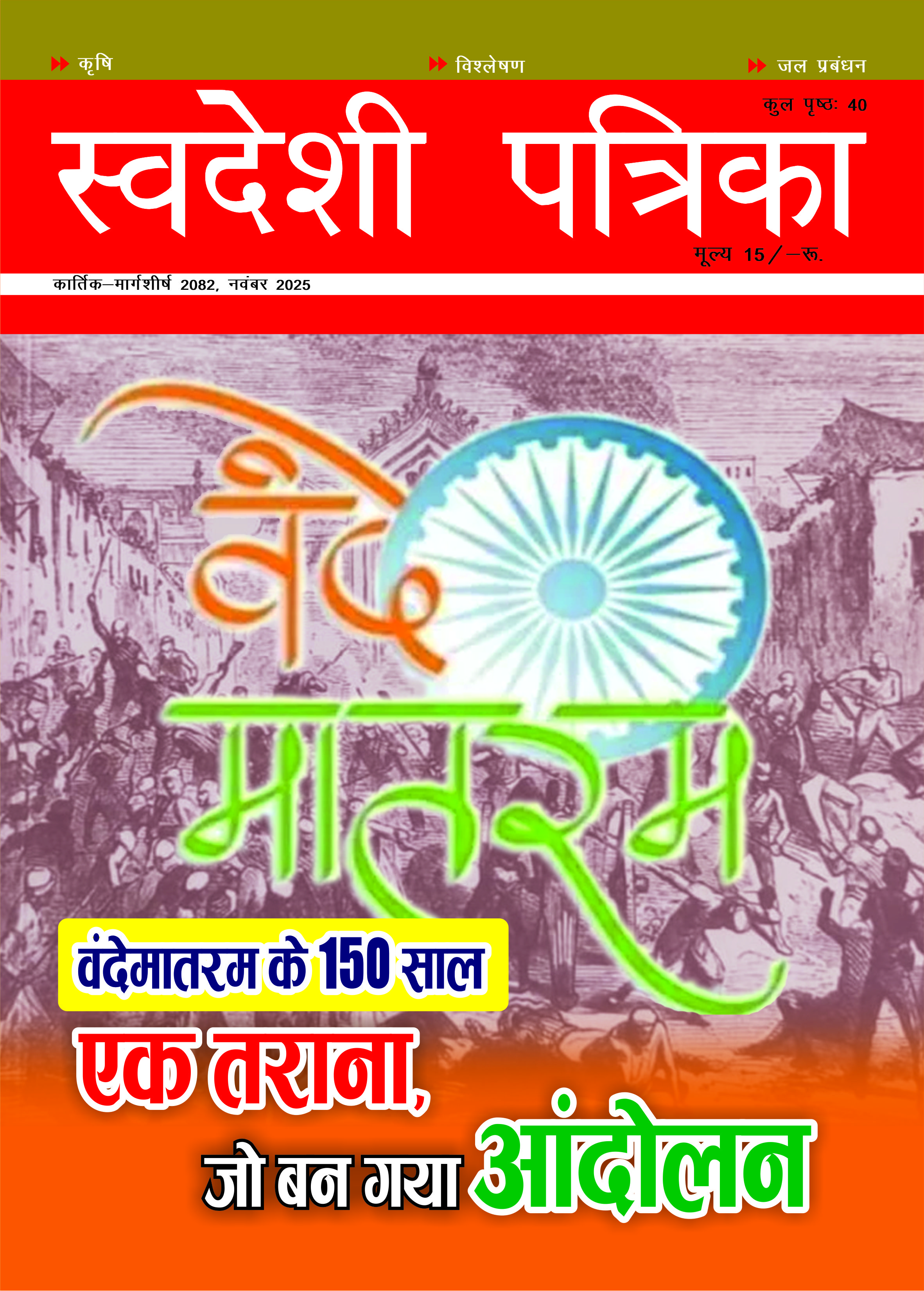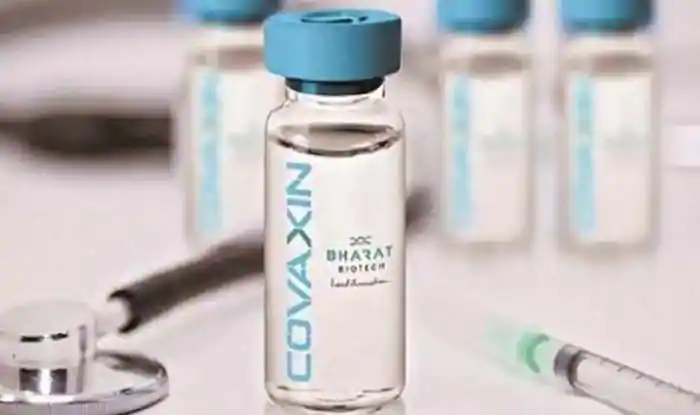
इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा तय हो
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह अस्पतालों में इलाज की कीमतों पर सीमा तय करें। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना के अंतर्गत इलाज प्रदान कर रहे अस्पतालों और नर्सिंग होमों के लिए विभिन्न इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा तय की भी है, लेकिन आमजन के लिए अस्पतालों पर कोई अंकुश नहीं है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को दिए निर्देश का खासा महत्व माना जा रहा है।
पिछले काफी समय से स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती जा रही है। पिछले लगभग 30 वर्षों में भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण की नीति के अंतर्गत एक ओर सरकारों के आर्थिक संसाधन सिकुड़े, तो दूसरी ओर सामाजिक सेवाओं की ओर सरकारों का नजरिया भी बदला। अब शिक्षा और स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सेवाओं पर कुल सरकारी खर्च के प्रतिशत के रूप में ठहराव आ गया है। लेकिन इस बीच बढ़ती संक्रामक एवं गैर संक्रामक बीमारियों, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बदलते नजरिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई शोध के कारण नई दवाइयों एवं जांच तथा नए इलाजों के अविष्कारों के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी ओर सरकारी सुविधाओं का विस्तार लगभग थम सा गया है। ऐसे में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की पूर्ति काफी हद तक अब निजी क्षेत्र से हो रही है।
इसके बावजूद अभी भी बाहरी रोगियों के मामले में 25 प्रतिशत और अस्पताल भर्ती के मामले में 40 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी संस्थानों से प्राप्त हो रही हैं। देखा जाए तो गांवों और शहरों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में इलाज, टीकाकरण, जच्चा-बच्चा देखभाल, समेत कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आमजन को प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र का बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए इजादों को गांवों और शहरों में आमजन तक पहुंचा पाया। इसका लाभ यह हुआ कि 5 वर्ष के नीचे के बच्चों की मृत्यु दर हाल ही के दशकों में खासी कम हुई है। गौरतलब है कि है यह दर घटती हुई 1992-93 में 119, 1998-99 में 101, 2005-06 में 74 और 2019 में मात्र 34 प्रति हजार ही रह गई है।
गौरतलब है कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी मोटे तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए भोजन की उपलब्धता, आदि के कारण है। प्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र का योगदान इस मामले में अधिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ सुविधाओं में अति अल्प विस्तार दिखाई देता है। सभी प्रांतों में नए बड़े अस्पताल, एम्स आदि स्थापित तो हुए हैं, लेकिन द्वितीयक/तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार अधिकांशतः निजी क्षेत्र और उनमें भी कारपोरेट क्षेत्र में हुआ है। बड़ी संख्या में छोटे-बड़े नर्सिंग होम भी निजी क्षेत्र में ही बने हैं।
बीमारियों के बढ़ने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और इलाज से संबंधित नए उपायों के चलते, देश में नर्सिंग होम अस्पताल में अधिक लोग भर्ती होते हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च वर्ष 2004 और 2014 के बीच लगभग ढ़ाई गुना से अधिक हो चुका है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान (एनएसएसओ) के 75वें सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक बार निजी क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 27347 रूपए और शहरी क्षेत्र में 38822 रूपए औसतन रिकार्ड किया गया (जूलाई 2017 से जून 2018)।
स्वास्थ्य के बढ़ते निजीकरण का असर यह हो रहा है कि जनता पर स्वास्थ्य खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। आज कुल स्वास्थ्य पर खर्च का दो तिहाई से ज्यादा जनता की जेब से होता है। ‘लैनसेट’ नामक मेडिकल जनरल के अनुसार भारत में लोग स्वास्थ्य पर अपनी जेब से 78 प्रतिशत खर्च करते हैं, जो कि दुनिया के अन्य मुल्कों से ज्यादा है। स्वास्थ्य खर्च के बोझ के कारण लोग गरीबी की रेखा से नीचे खिसकते जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में सरकार ने 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रूपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए इलाज का बोझ अभी भी असहनीय है।
निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य क्षेत्र (विशेष तौर पर द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं) में बढ़ती भूमिका और आमजन पर बढ़ते दबाव के चलते निजी क्षेत्र के नियमन की जरूरत बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने हृदय की धंमनियों में लगने वाले स्टंट और कृत्रिम घुटनों की कीमतों को नियंत्रित कर आम जनता को बड़ी राहत दी थी, लेकिन इतना भर करना अत्यंत अपर्याप्त माना जा रहा है। इसलिए सभी के लिए और सब प्रकार के इलाज की दरें नियमित करना समय की मांग है।
दवाइयों के क्षेत्र में अति आवश्यक दवाइयों में कीमत नियंत्रण हेतु नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) कार्यरत है। इस संस्थान द्वारा चिकित्सा खर्च का नियमन किया जाता है। इस संबंध में कई उपकरणों को पहले से ही दवा की श्रेणी में रखकर उनकी कीमत नियंत्रण हेतु आधार बन चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि निजी क्षेत्र में चिकित्सा लागत को नियंत्रित करने हेतु एक नियामक प्राधिकरण बने, जो समय-समय पर विभिन्न इलाजों के लिए उपयुक्त कीमत निर्धारण करने का कार्य करें। आमजन को निजी क्षेत्र द्वारा अनुचित शोषण से बचाने के लिए यह एक जरूरी कदम होगा।