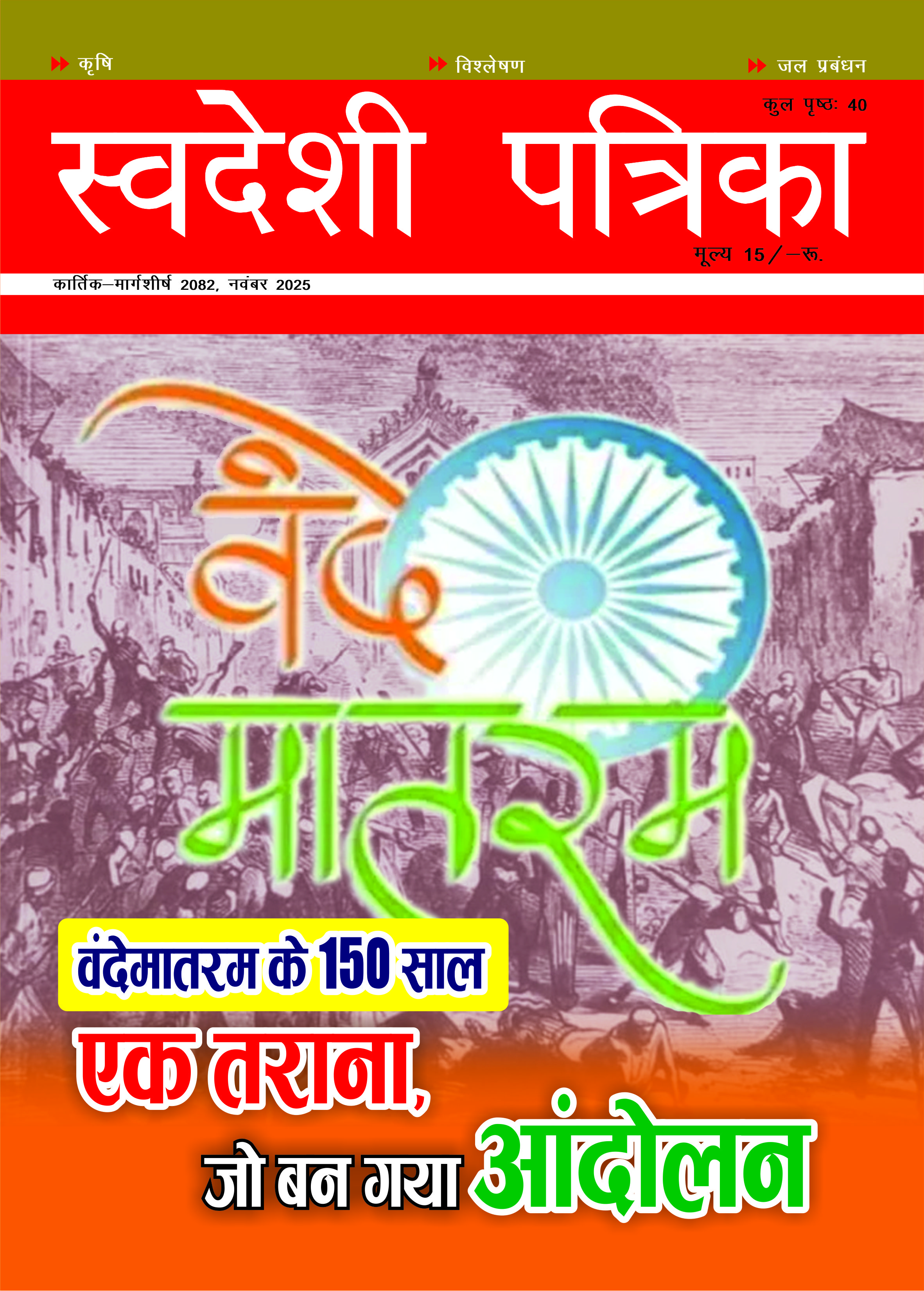सरकारी बैंकों के निजीकरण पर उठते सवाल
इस वर्ष के आम बजट में वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि दो सरकारी बैंकों और एक सरकारी बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान कानूनों के अनुसार सरकारी बैंकों में केन्द्र सरकार की 51 प्रतिशत भागीदारी अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान घोषित नीति के अनुसार सरकार की मंशा सरकारी बैंकों के निजीकरण के बाद अपनी भागीदारी शून्य करने की है। इसी मंशा को लागू करने के लिए बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को 2021 के शीतकालीन सत्र में सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन किसी कारण से उसे प्रस्तुत नहीं किया गया। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकोनोमिक रिसर्च की महानिदेशक पूनम गुप्ता और कोलंबिया विश्वविद्यालय के अरविन्द पनगरिया, जो नीति आयोग के पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, द्वारा एक अकादमिक लेख प्रकाशित करने के बाद सरकारी बैंकों के निजीकरण की बहस और तेज हो गई है। निजीकरण के हिमायती दोनों लेखों के इस लेख में सिफारिश की गई थी कि केवल भारतीय स्टेट बैंक को सरकारी हाथों में रखते हुए शेष सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए। सरकारी बैंकों के निजीकरण के समर्थकों के तर्क कई कारणों से औचित्यपूर्ण नहीं ठहराए जा सकते। 1969 में जब पहली बार 14 निजी बैंकों का और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय उसका मुख्य उद्देश्य सर्वसमावेशी विकास को बढ़ावा देना था। कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा, निर्यात संवर्धन आदि को प्राथमिक महत्व का मानते हुए उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से साख की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। इसके अलावा अति सूक्ष्म ऋणों के लिए अत्यंत कम ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता भी सार्वजनिक बैंकों से ही सुनिश्चित हुई थी। हालांकि तब से अभी तक परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निजी बैंकों को भी राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि तमाम नियमों, उपनियमों और निर्देशों के बावजूद सर्वसमावेशी विकास हेतु जितना काम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक करते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक नहीं करते। नरेन्द्र मोदी सरकार के आने के बाद वित्तीय समावेश के उद्देश्य से जीरो बैंलेंस वाले जनधन खाते खोले गए। अभी तक ऐसे 46 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिसके माध्यम से न केवल गरीब, आमजन की बैंकों तक पहुंच बन पाई है, बल्कि सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इन्हीं जनधन खातों, जो आधार और मोबाईल फोन के साथ जुड़े हैं, संभव हुआ है। किसान निधि का अंतरण हो अथवा 20 करोड़ महिलाओं को कोविड संबंधित नकद का अंतरण, यह सभी प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण ही हो पाया है। लेकिन आज जब निजी बैंकों का जमा और उधार में हिस्सा लगभग 37 प्रतिशत है, मात्र 10 प्रतिशत जनधन खाते ही निजी बैंकों द्वारा खोले गए। यही नहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 6 करोड़ महिलाओं को जीविका ऋण देने में भी सरकारी बैंकों और उन बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 90 प्रतिशत ऋण प्रदान किए गए। इसी प्रकार अति लघु उद्यमों और व्यापारियों को ऋण देने का काम भी सरकारी बैंकों द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में स्वभाविक तौर पर निजी क्षेत्र के बैंकों के लाभ सरकारी बैंकों से ज्यादा होंगे ही, क्योंकि ये बैंक वित्तीय समावेशन के काम से कन्नी काट लेते हैं। सरकारी बैंकों को सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने की बाध्यता रहती ही है, ऐसे में निजी क्षेत्रों के बैंकों को इसलिए सक्षम मान लेना कि वे लाभ ज्यादा कमा रहे हैं, उचित नहीं होगा। यदि सरकारी बैंकों के कामकाज में से वित्तीय समावेशन और सोशल बैंकिंग हटा दी जाए, तो उनके भी लाभ निजी बैंकों जैसे ही बढ़ सकते हैं।
रिज़र्व बैंक का पहले यह तर्क रहा है कि उसके पास सरकारी बैंकों के मामले में नियमन के ज्यादा अधिकार नहीं हैं और इसलिए वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता है, जबकि निजी बैंकों पर उसका नियंत्रण है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है। आरबीआई के पास सरकारी बैकों पर नियंत्रण और नियमन की कई शक्तियां हैं, जिसमें नियुक्तियां, लेखा परीक्षा और ऋण पर नीति आदि शामिल हैं। जहां तक सरकारी बैंकों के एनपीए का सवाल है, यह सर्वविदित ही है कि यूपीए शासन के दौरान वर्ष 2004 से 2014 के बीच के एक दशक में इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋणों के नाम पर बड़े ऋण दिए गए और उनमें से भारी मात्रा में ये ऋण डूबे भी। किसी न किसी रूप से इन डूबे ऋणों की वसूली हेतु नियमों में बदलाव करते हुए और नया दिवालिया कानून बनाया गया। लेकिन इसके कारण सरकारी बैंकों का काफी पैसा डूब गया। चूंकि अब नियमों को सख्त बनाया गया है और भविष्य में इस प्रकार की गलतियों के दोहराए जाने की संभावनाएं बहुत सीमित हैं, सरकारी बैंकों द्वारा की जा रही सोशल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के मद्देनजर सरकारी बैंकों का निजीकरण नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि इस संबंद्ध में कोई ठोस तर्क नहीं है, लेकिन बैंकों के निजीकरण के समर्थक यह तर्क देते हैं कि यदि देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो उसके लिए सरकारी बैंकों का निजीकरण जरूरी है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों सरकारी बैंक सौंपने के बारे में मतैक्य नहीं है। देश के निजी बैंकों के प्रमोटरों की हैसियत नहीं है कि वे सरकारी बैंकों को खरीद सकें तो ऐसे में इस बात का खतरा भी है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण करने पर बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रादुर्भाव बढ़ेगा। इसका नुकसान देश को हो सकता है। सरकारी बैंकों में केन्द्र सरकार के प्रश्रय के कारण कोई सरकारी बैंक नहीं डूबा, लेकिन इस बीच में कई बार कई निजी बैंकों को सरकारी बैंकों और हस्तक्षेप के द्वारा डूबने से बचाया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व कई निजी बैंक डूबे जिसके कारण आम जनता को खासा नुकसान हुआ। हाल ही में लक्ष्मी विलास नामक एक निजी बैंक को सिंगापुर के एक बैंक के हवाले करना पड़ा था। ऐसे में यदि बैंकों के निजीकरण के चलते यदि देश का वित्तीय क्षेत्र विदेशी आधिपत्य में चला जाता है तो उसके दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था को भुगतने पड़ेंगे। इसलिए सरकारी बैंकों के निजीकरण को केवल कुछ संस्थाओं अथवा कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर अंजाम देना उचित नहीं होगा। इसके कारण होने वाले बदलावों और संभावित दुष्प्रर्भावों के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है।