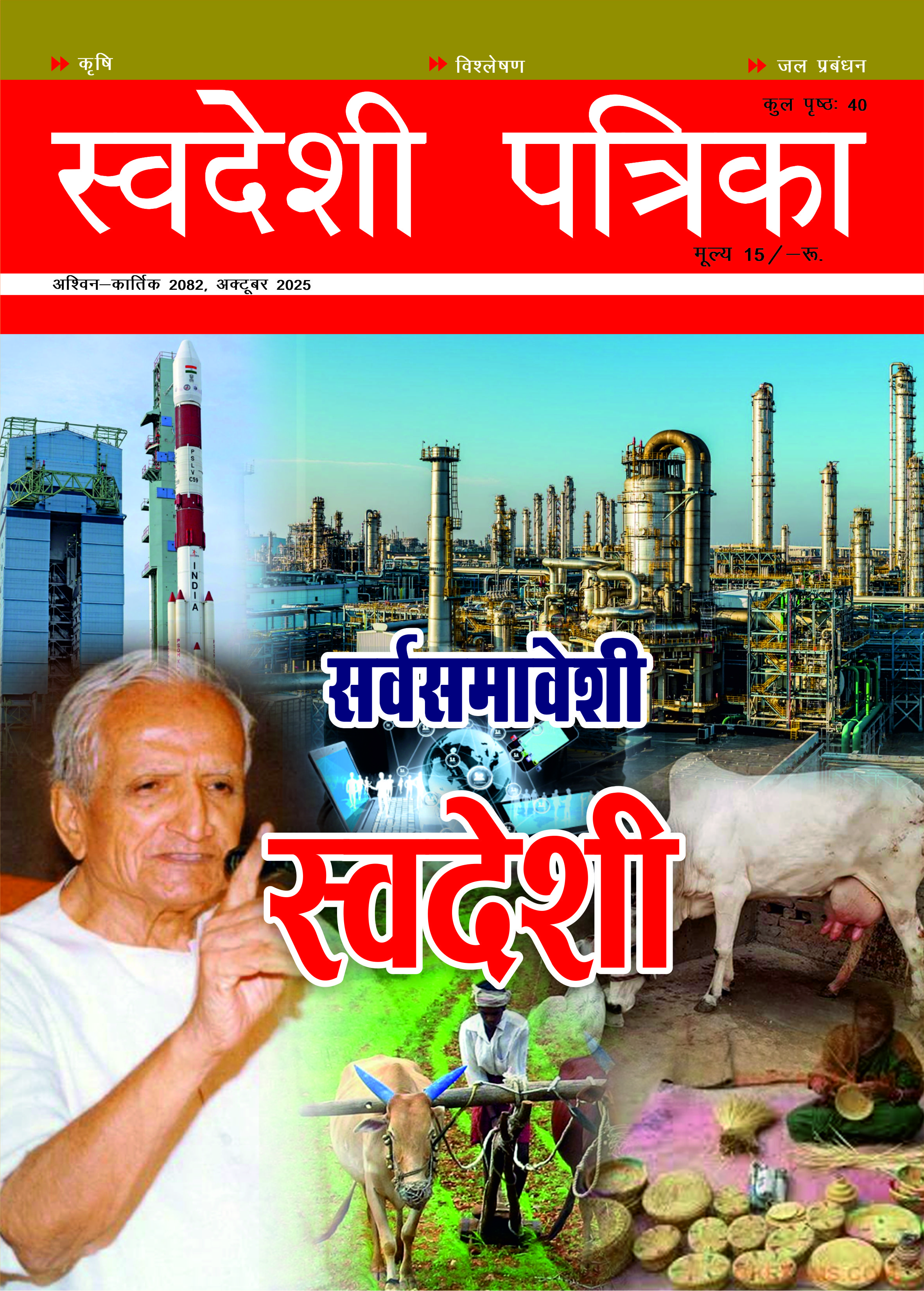कृषि एवं स्वदेशी दृष्टि
आज भारत में प्रति व्यक्ति अन्नोत्पादन विश्व के प्रायः अन्य देशों की तुलना में कम है। अतः स्वदेशी कृषि का पहला लक्ष्य तो देश में अन्नोत्पादन की मात्रा को शीघ्रातिशीघ्र बढ़ाना चाहिए। - शिवनंदन लाल
भारतीय संस्कृति में कृषि की बहुत महत्ता है। दशावतारों में से एक भगवान श्री बलराम हल एवं मूसल धारण किया करते थे और परब्रह्म परमात्मा स्वयं श्रीकृष्ण हल मूसलधारी कृषक श्रीबलराम के रूप में अवतरित हुए थे। भारतीय परम्परा के गहनतम विद्वान राजा जनक अपने हाथ से हल चलाते थे। हल लेकर यज्ञार्थ पृथ्वी का कर्षण करते हुए ही राजा जनक को सीता जैसी पुत्री प्राप्त हुई थीं और, कृषि के माध्यम से प्राप्त पृथ्वी-पुत्री जानकी (सीता) से विवाह कर पुरुषोत्तम श्रीराम संपूर्ण हुए थे। अपने कलियुग में श्री गुरुनानक ज्ञान के अनुसंधान में अनेक बार विश्वाटन करते रहे और अंततः ब्रह्मतत्व को प्राप्त करने के उपरांत वे करतारपुर में बसकर कृषि करने लगे। वहां करतारपुर में कृषि करते हुए श्री गुरुनानक ने सिक्ख संप्रदाय की स्थापना की। उनके साथ मिलकर कृषि करते हुए ही भाई लहना गुरुपद को प्राप्त हुए और इस प्रकार सिक्ख गुरु परंपरा का सूत्रपात हुआ। यह स्वाभाविक ही है कि श्रीगुरुनानक के अनुयायी सिक्ख आज भी देश के सर्वोत्तम कृषकों में गिने जाते हैं।
महाभारत के शांतिपर्व में युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हुए भीष्म पितामह उन्हें बताते हैं कि ’निश्चय ही कृषक राजा का बोझ अपने कंधों पर उठाते हैं। कृषक ही राष्ट्र में अन्य सबका भरण करते हैं। कृषकों के दिए अन्न से ही देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस, पशु एवं पक्षी सब-के-सब जीवन धारण करते हैं। अतः राजा को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कृषक पीड़ित हों।’ इसी प्रकार सभापर्व में नारदमुनि राज्य की व्यवस्था के विषय में युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हुए कृषि के प्रति विशेष आग्रहपूर्वक जानना चाहते हैं कि ’तुम्हारे राज्य में किसान संतुष्ट तो हैं? राज्य के सब भागों में खेतों की सिंचाई के लिए विशाल तड़ाग तो बना दिए गए हैं न? ये सब तड़ाग जल से परिपूर्ण तो रहते हैं? कहीं कृषि मात्र वर्षा के जल पर निर्भर तो नहीं? खेती को मात्र दैव पर ही तो नहीं छोड़ दिया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे राज्य के कृषक अन्न अथवा बीज के अभाव में कष्ट पा रहे हों? ऐसी स्थिति में तुम उन पर अनुग्रह कर एक प्रतिशत व्याज पर ऋण तो दिया करते हो न?’ आदि।
वाल्मीकि रामायण में जब भरत श्रीराम को मिलने चित्रकूट जाते हैं तो कोशल देश की सुव्यवस्था के प्रति चिंतित श्रीराम भरत से कृषि संबंधी ऐसे ही अनेक प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि कोशल देश के तड़ाग जल से परिपूर्ण तो हैं, कृषि मात्र बरसा पर तो निर्भर नहीं हो गयी, देश कृषि में समर्थ स्वस्थ पशुओं से परिपूर्ण तो है, आदि। और अंत में वह भरत से पूछते हैं कि ’कृषि एवं गोरक्षा ही जिनका जीवन है. ऐसे सब लोग तुम्हारे विशेष प्रीतिपात्र तो हैं न? कृषि एवं गोरक्षा का अवलम्बन लेकर ही यह लोक सुख-समृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए इन कार्यों में लगे लोगों का तुम्हें विशेष सावधानीपूर्वक भरण करना चाहिए। इनके दृष्टि की प्रति एवं अनिष्ट के निवारण के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।’
भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में कृषि का ऊँचा महत्व रहा है। अतः कृषि के प्रति स्वदेशी दृष्टि का पहला आयाम तो यही है कि देश की नीति में कृषि को वैसा ही उच्च स्थान प्राप्त हो जैसा भारतीय परंपरा में उसे दिया गया है।
महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय जब स्वदेशी का आंदोलन चलाया था तो खादी को स्वदेशी का मूलाधार बनाया था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ वर्ष पूर्व भविष्य के भारत पर विचार करते हुए उन्होंने अनेक बार स्पष्ट किया था कि खेती पर वे इसलिए आग्रह नहीं कर पाये क्योंकि खेती के उन्नयन के लिए राज्य का सहयोग आवश्यक होता है। विदेशी राज तो खेती में होने वाले किसी सुधार का लाभ कृषकों तक पहुंचने ही नहीं देता।
गांधी जी ने कहा था कि खादी हमें उतना आगे नहीं ले जा सकती जितना हम सोचते रहे हैं। तो हमें कृषि जैसे किसी अन्य मूलभूत व्यवसाय को अपनाने पर विचार करना चाहिए। मेरा तो प्रारंभ से ही यह पक्का विश्वास रहा है कि कृषि ही इस देश के लोगों के भरण-पोषण का स्थायी एवं अचूक साधन बन सकती है।
विदेशी प्रशासन के अधीन खेती को भारत की जागृति एवं भारत के गांवों की उन्नति का मूलाधार बनाने में महात्मा गांधी हिचक रहे थे। परंतु स्वतंत्र भारत में राष्ट्र-निर्माण का मूलाधार तो उनके अनुसार कृषि को ही होना था।
भारत के लोकजीवन में कृषि के स्थान पर विशेष चिंतन हुआ है। परंतु जहां ऐसे गहन चिंतन की परंपरा नहीं है वहां भी कृषि को आर्थिकता का मूल तो माना ही जाता है। एडम स्मिथ का समस्त चिंतन स्वदेशी के विपर्याय-सा है। परंतु उनका भी मानना है कि अन्न उत्पादन की प्रचुरता के बिना किसी समाज की अर्थव्यवस्था का प्रारंभ ही नहीं होता। वे कहते हैं कि “जब अन्न पर्याप्त होता है तभी अन्य वस्तुओं का मूल्य लगना शुरू होता है। जहां अन्न ही पर्याप्त न हो वहां तो रोटी के टुकड़े के बदले में सोना प्राप्त किया जा सकता है।
एशिया के जिन देशों को प्रायः हमारे साथ-साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उनमें से अधिकतर ने राष्ट्र निर्माण में कृषि की मौलिक स्थिति को समझा है। इण्डोनेशिया, थाइलैंड, ताईवान, दक्षिण कोरिया में भी कृषि ही राष्ट्रीय विकास का ध्येय बना। कृषि के मार्ग पर चलकर ही औद्योगीकरण की ओर बढ़े।
आज वैश्वीकरण के युग में राष्ट्र विकास का मूलाधार कृषि को बनाना और आवश्यक हो गया है। कृषि के उन्नयन में किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को वह दृढ़ता प्राप्त होती है जो उसे समर्थ बनाती है। चीन ने इस मूल सिद्धांत को समझते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के खुला छोडने से पूर्व अपनी कृषि को बढ़ाया। ऐसे ही वियतनाम ने अपना सारा ध्यान कृषि की वृद्धि पर केंद्रित किया।
आज भारत में प्रति व्यक्ति अन्नोत्पादन विश्व के प्रायः अन्य देशों की तुलना में कम है। अतः स्वदेशी कृषि का पहला लक्ष्य तो देश में अन्नोत्पादन की मात्रा को शीघ्रातिशीघ्र बढ़ाना चाहिए। वस्तुतः राज्य को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि कृषक अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करने की ओर प्रवृत्त हो।
भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गयी है। उपनिषद् का आदर्श वाक्य हैः अन्नं बहुकुर्वीत। सब प्रकार से अन्न का बाहुल्य करो। अन्न संबंधी इस भारतीय परंपरा को परिभाषित करते हुए ही जगद्गुरु श्री शृङ्गेरी आचार्य श्रीमद्भारती तीर्थ महास्वामी ने कहा था कि अन्न का सम्यक् उत्पादन एवं विनियोग किए बिना कोई राष्ट्र अन्यान्य विषयों में परिश्रमशील होने लगे, यह तो ऐसे हुआ जैसे कोई व्यक्ति उपनयन किए बिना ही वाजपेय आदि यज्ञों का संपादन करने का प्रयास करने लगे। यह असंभव है।
भारतीय परंपरा में अन्न के उत्पादन का जैसा महत्व है उससे कहीं अधिक अन्न के सम्यक् विभाजन का है। भारत के सामान्य -जन आज भी ऐसा मानते हैं कि जहां अन्न का सम्यक् विभाजन नहीं होता वहां सम्यक् उत्पादन भी नहीं हो पाता। रामचंद्र जी अपने वनवास के दिनों में लक्ष्मण के साथ अन्न का अनुसंधान करते हुए घूम रहे थे। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि देखो यह सारी पृथ्वी धन-धान्य से परिपूर्ण है. परंतु हमें भोजन प्राप्त करने के लिए दौड़-धूप करनी पड़ रही है। इस समस्या का समाधान करते हुए आगे वे लक्ष्मण को बताते हैं कि पूर्वकाल में हमने पर्याप्त अनुदान नहीं किया होगा, तभी हमें अन्न के लिए इस प्रकार भटकना पड़ रहा है। क्योंकि यह नियम है कि अन्न तो उतना ही प्राप्त होता है जितना अन्यों को देकर अर्जित कर लिया जाता है। और, सम्यक् विभाजन से जो अर्जित नहीं कर लिया गया उसे तो न विद्या से और न पौरुष से पाया जा सकता है।
जिस नियम का अतिक्रमण श्रीरामचन्द्र जी से संभव नहीं था, उसका सामान्यजन कैसे अतिक्रमण करेंगे? इसीलिए भारत के धर्मशास्त्रों की यह स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी गृही को अन्न का उपभोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सब जीव, सब मानव, पशु, पक्षी और देव, गंधर्व, पितरादि सब तृप्त हो चुके हैं। सबको अपना-अपना भाग प्राप्त हो चुका है। महाभारत में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में किसी एक भी जीव को भूख की पीड़ा सहने को विवश होना पड़ता है, उस राजा का जीना व्यर्थ है। ऐसी परम्परा वाले देश में स्वदेशी कृषि नीति निश्चय ही अनाज के सम्यक् संविभाजन पर आधारित होगी।