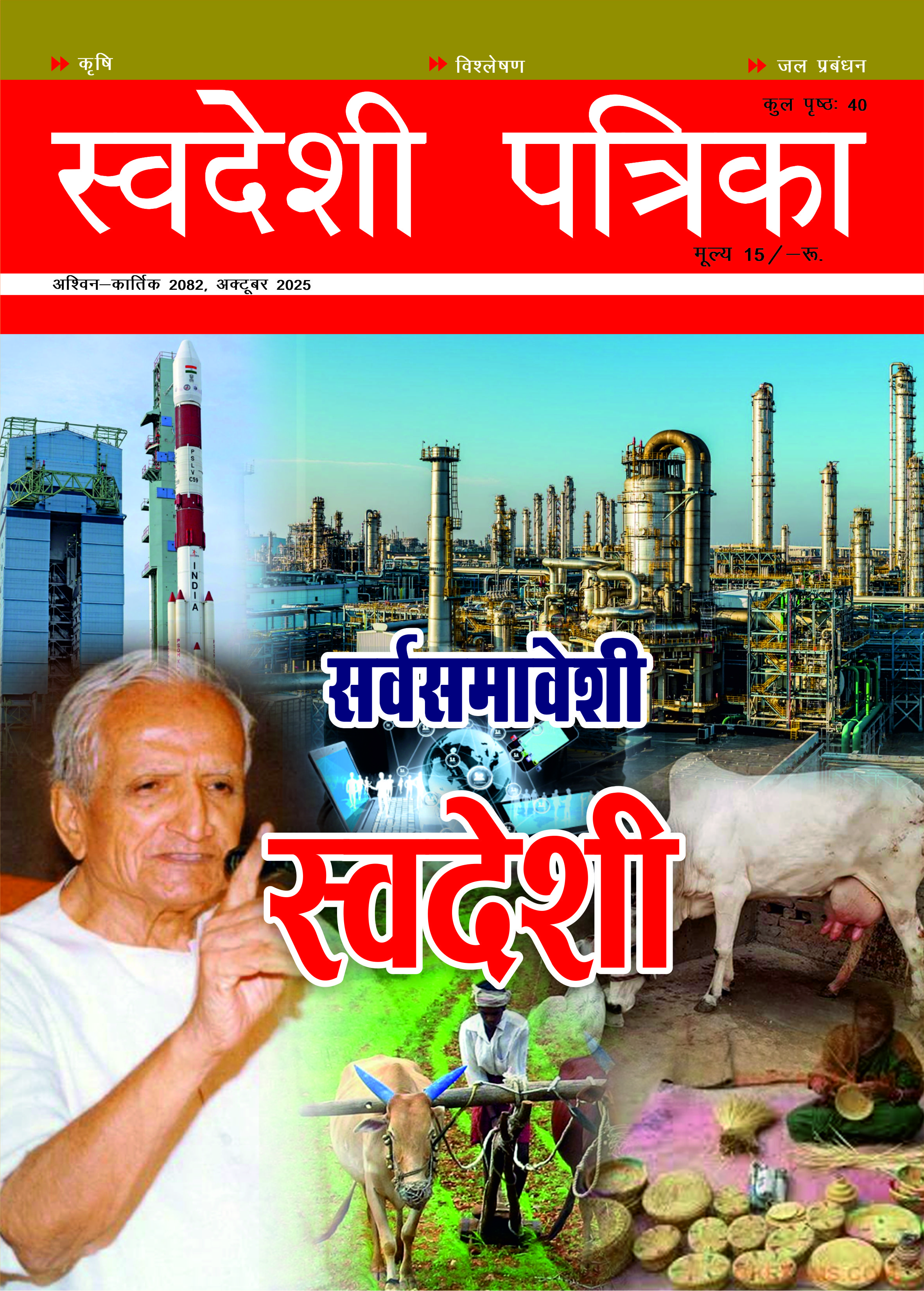भारत-अमेरिका टैरिफ़ युद्ध का द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव
भारत-अमेरिका टैरिफ युद्ध ने अल्पावधि में व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा किया है। इस व्यवधान के समाधान के लिए बहुपक्षीय वार्ता, पारदर्शी नीति और संतुलित शुल्क प्रणाली आवश्यक है। - दुलीचंद कालीरमन
भारत और अमेरिका दोनों ही बड़े लोकतान्त्रिक देश और वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके अतिरिक्त वैश्विक शक्ति-संतुलन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक दुसरे के अहम् सांझेदार भी है। पिछले दो दशकों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक एवं रणनीतिक संबंध तेज़ी से बढ़े हैं लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ़ (शुल्क) नीतियों ने व्यापारिक रिश्तों के साथ-साथ रणनीतिक संबंधों में भी खटास पैदा कर दी है।
हांलाकि टैरिफ़ युद्ध की शुरुआत डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति के रूप में पहले कार्यकाल में 2018 के बाद हो गई थी जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ बढ़ाए थे और भारत ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। भारत को अमेरिका से टैरिफ़ के मामले में टकराहट का अंदेशा उसी समय हो गया था जब अमेरिकी प्रशासन ने “अमेरिका प्रथम” नीति के तहत अपने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात शुल्क बढ़ा दिए। भारत ने भी अमेरिकी बादाम, अखरोट, सेब, मोटरसाइकिल पार्ट्स आदि पर अतिरिक्त शुल्क लगाए। 2019 में अमेरिका ने भारत को दिए गए सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जी.एस.पी.) लाभ समाप्त कर दिए, जिससे लगभग $5.6 बिलियन मूल्य के भारतीय निर्यात प्रभावित हुए। सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली एक अमेरिकी व्यापार नीति है जो विकसित देश विकासशील देशों को कुछ उत्पादों पर शुल्क में छूट या कमी प्रदान करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था।
डोनाल्ड ट्रम्प लंबे समय से भारत को “टैरिफ किंग” कहकर बदनाम कर रहे है। अमेरिकी सरकार के अनुसार, 2024 में भारत से व्यापार में उसे 45.8 अरब डॉलर का भारी व्यापार घाटा हुआ लेकिन यह आंकड़ा सही नहीं है क्योंकि अगर हम अमेरिकी तकनीकी कंपनियों द्वारा भारत से कमाये जाने वाले राजस्व और अन्य मदों की आय को जोड़ दें तो यह आंकड़ा अमेरिका के पक्ष में जाता है। भारत से अमेरिका को मुख्यत फ़ार्मास्यूटिकल्स (दवाइयाँ), वस्त्र और रेडीमेड कपड़े, हीरे-गहने, सॉफ़्टवेयर और सॉफ्टवेर सेवाएँ, औद्योगिक मशीनरी निर्यात की जाती है जबकि अमेरिका से भारत कच्चा तेल और एलएनजी, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण, मशीनरी, मेडिकल उपकरण, कृषि उत्पाद (सोयाबीन, बादाम, आदि) आयात करता है। अमेरिका भारत पर कृषि और डेयरी क्षेत्र को अनुमति देने का दबाव बना रहा है जबकि भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करने से इनकार कर दिया है क्योकि ये क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।
अमेरिका द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात का बहाना बनाकर भारत पर दबाव डालने के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। जबकि भारत ने रूस से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदकर वैश्विक स्तर पर डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बनाया था, जिसकी वजह से वैश्विक तेल की कीमतें ज्यादा ऊपर नहीं जा पाईं थीं। यह भारत द्वारा लिए गया एक रणनीतिक कदम था। ट्रंप के अनुसार भारत का यह कदम न्यायापूर्ण नहीं था। हालांकि भारत ने साफ किया कि दूसरे देशों को नजरअंदाज करके केवल भारत पर निशाना साधना बेबुनियाद है। भारत का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के साथ यूरेनियम और पैलेडियम जैसे सामानों का व्यापार जारी रखे हुए हैं। जबकि भारत पर रूस से तेल आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर दण्डित करने का प्रयास हुआ हैं। ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत और रूस के गहरे होते ऊर्जा संबंध अमेरिका के हिंद-प्रशांत रणनीति में उसकी भूमिका से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं।
दरअसल यह ट्रेड वॉर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण, दीर्घकालिक स्तंभ हैं। इसके 60 प्रतिशत से अधिक सैन्य उपकरण रूस से आयात होते हैं। यह निर्भरता भारत के लिए रूस को एक महत्पूर्ण रणनीतिक साझेदार बनाती है। ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ को व्यापक रूप से “भू-राजनीतिक दबाव” की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। भारत पर दीर्घकालिक सहयोगी रूस से संबंध जारी रखने या अमेरिका के साथ अपने संबंधों का चयन करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। ताकि भारत को रूस से दूर करके रूस-यूक्रेन युद्ध का अपनी शर्तों पर युद्धविराम करवाया जा सके।
हालाँकि अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद ने व्यापार में चुनौतियाँ पैदा कीं, लेकिन रक्षा और तकनीकी सहयोग पर इनका ज्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ा। भारत और अमेरिका दोनों देश चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क हैं, इसलिए रणनीतिक साझेदारी अभी भी बनी हुई है। यदि यह टैरिफ विवाद लंबे समय तक चलता रहा तो यह निवेश प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग, और स्टार्टअप-टेक सेक्टर पर नकारात्मक असर डाल सकता है। लेकिन अगर भारत और अमेरिका में व्यापार समझौता हो जाता है तो यह व्यापारिक विश्वास को मज़बूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार को $200 बिलियन से ऊपर ले जा सकता है। पिछले कुछ समय में टैरिफ विवाद के कारण कुछ सेक्टर्स (जैसे कृषि उत्पाद, स्टील, वस्त्र) में निर्यात-आयात वृद्धि की गति धीमी हुई। भारत ने अभी से वैकल्पिक बाजारों (जैसे अफ्रीका, यूरोप, ब्रिटेन, आशियान) की ओर ध्यान बढ़ाया है।
भारत के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई बिना सोचे-समझे लिया गया फैसला है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका उद्देश्य एक राजनीतिक एजेंडा सेट करना है। भारत पर लगाया गया दंडात्मक शुल्क दोनों देशों के बीच पिछले दो दशकों की कड़ी मेहनत से बनाए गए विश्वास और सहयोग को खतरे में डाल रहे हैं। ट्रंप के पुराने सहयोगी भी उनके इस फैसले से सहमत नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन ने भारत के साथ टैरिफ प्रकरण पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि अमेरिका ने भारत को रूस और चीन से दूर करने के दशकों पहले से चले आ रहे प्रयासों को खतरे में डाल दिया है।
भारत-अमेरिका टैरिफ युद्ध ने अल्पावधि में व्यापारिक रिश्तों में तनाव पैदा किया है। इस व्यवधान के समाधान के लिए बहुपक्षीय वार्ता, पारदर्शी नीति और संतुलित शुल्क प्रणाली आवश्यक है। इससे भी अधिक बराबरी पर आधारित रिश्ते एवं अमेरिका को खुद को ‘विश्व का दरोगा’ समझने की चेष्टा को त्यागना होगा। अमेरिका को भारत के प्रति अपना पुराना नज़रिया बदलना होगा तथा विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था और सबसे तेजी से विकास के पथ पर बढते नए भारत के साथ समानता के धरातल पर वार्ता करनी होगी।