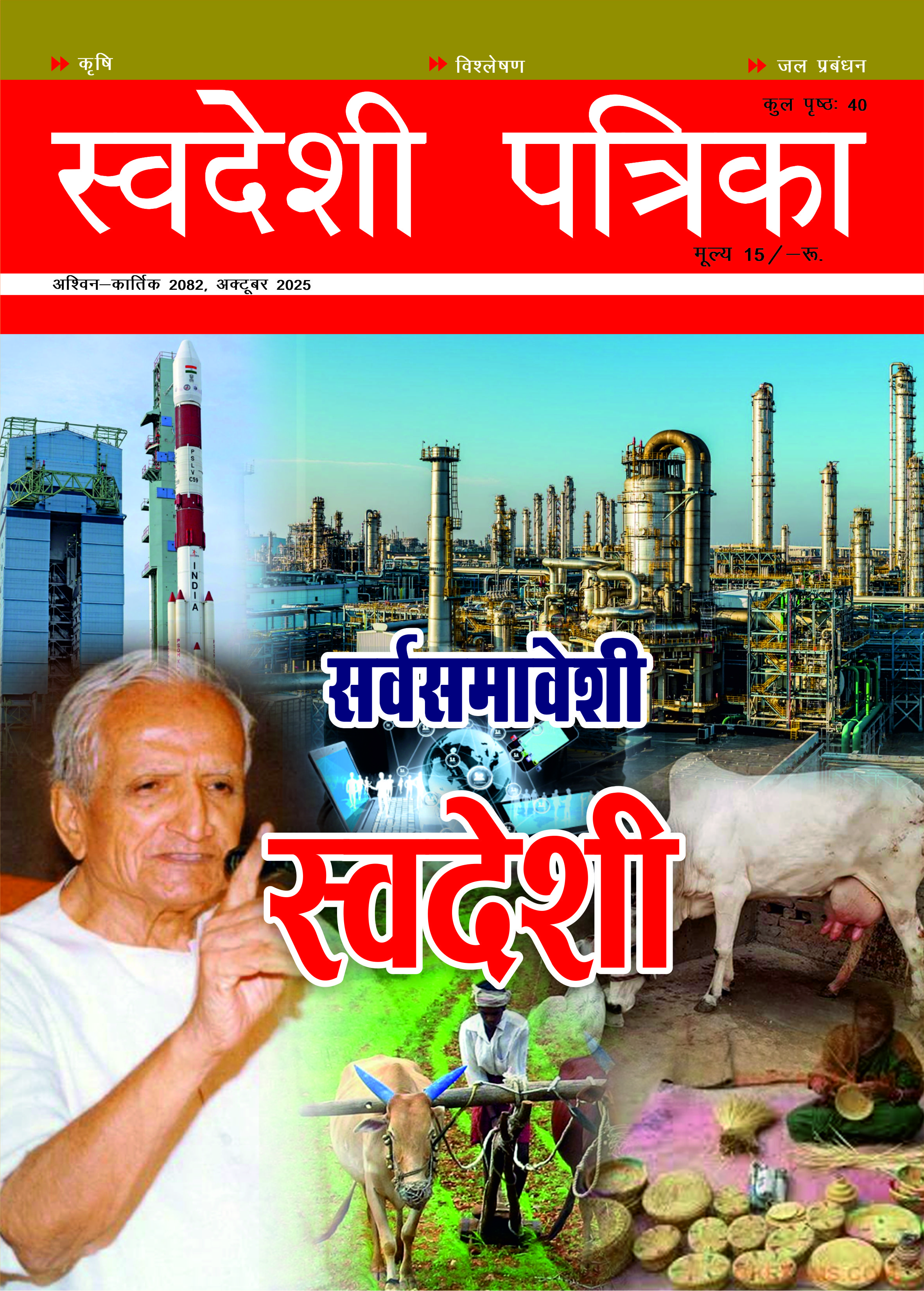भारत बना दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश
असमानताओं का आकलन करने वाले घरेलू सर्वेक्षणों की कमियों और कमज़ोरियों को तो समझा जा सकता है, लेकिन गरीबी में निश्चित रूप से कमी आई है, चाहे वह चरम पर हो या बहुआयामी। — डॉ. अश्वनी महाजन
हाल ही में जारी विश्व बैंक की ‘स्प्रिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ’ ने दुनिया में एक बहस शुरू की है। बहस का मुद्दा यह है कि क्या भारत वास्तव में दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है? वास्तव में देश और दुनिया में प्रचलित विमर्श का यह रिपोर्ट खंडन करती है। देश में बड़ी तादाद में बुद्धिजीवी जो इससे पूर्व की रिपोर्टों और आंकड़ों का हवाला देते हुए यह तर्क देते रहे हैं कि देश में आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ असमानताएं भी बढ़ी है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ी है, वंचित वर्ग के हालात पहले से अधिक बिगड़े है और यह असमानता आय और संपत्ति दोनों में दिखाई देती है। ऐसे में यदि कोई रिपोर्ट यह कहे कि देश में असमानताएं कम हुई है तो असमंजस स्वाभाविक ही है। ऐसे में उन बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट पर प्रश्नचिन्ह लगाना भी स्वाभाविक ही है।
लेकिन यहां यह भी सत्य है कि जो लोग यह मानते हैं कि देश में आय और संपत्ति की असमानताएं बढ़ी है, वे भी आंकड़ों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं और जो रिपोर्ट विश्व बैंक ने प्रकाशित की है, वह भी आंकड़ों पर ही आधारित है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल है, जैसा उसके आलोचक दावा करते हैं या उसमें कुछ सच्चाई है। और यदि यह सच है तो यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में समानताएं घटने के पीछे प्रमुख कारण क्या हैं?
आय और संपत्ति की असमानताएं
असमानताओं को मापने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका गिनी चटांक माना जाता है। गिनी चटांक शून्य से एक तक होता है, जहां शून्य गिनी सह गुणांक पूर्णतः समानता को और एक पूर्णतः असमानता को दर्शाता है।
नेशनल काउंसिल ऑफ़ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च और अन्य गृहस्थ आय सर्वेक्षणों के आंकड़ों के अनुसार 2023 में आय गिनी सह गुणांक 0.410 था जो 1955 में 0.371 से भी अधिक था। यदि संपत्ति के वितरण के बारे में विचार करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2023 में यह सह गुणांक 0.405 था जो 1955 में 0.341 से कहीं अधिक था जबकि शहरी क्षेत्र में यह 1955 में 0.392 से घटकर 2023 में 0.382 ही रह गया लेकिन अभी भी यह काफी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है।
लेकिन घट गई है उपभोग में असमानताएं
भारत में आय और संपत्ति में बढ़ती असमानताओं के बीच, अच्छी खबर यह है कि उपभोग में असमानताएँ कम हो रही हैं। इसे अलग-अलग शब्दों में पहले यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में भारी कमी और बाद में विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में अत्यधिक गरीबी में बड़ी कमी दर्ज की गई है। हालाँकि अत्यधिक गरीबी की परिभाषा 2.15 डॉलर प्रतिदिन से बदलकर 3.0 डॉलर प्रतिदिन कर दी गई है, फिर भी 2022-23 में केवल 5.3 प्रतिशत लोग ही अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे। दिलचस्प बात यह है कि 2011-12 में यह आँकड़ा 27.1 प्रतिशत था। और यदि इस परिभाषा को पहले की तरह 2.15 डॉलर ही रखा जाए, तो 2022-23 में अत्यधिक गरीबी से पीड़ित लोगों का प्रतिशत केवल 2.3 प्रतिशत ही रह गया है।
विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में उपभोग में असमानताएँ अब कम हो गई हैं। एक अधिक समतापूर्ण समाज की ओर भारत की यात्रा पिछले कुछ वर्षों में उसके गिनी सूचकांक में परिलक्षित होती है। 2011 में यह सूचकांक 28.8 था, जो 2022 में 25.5 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि अब यूएनडीपी से लेकर विश्व बैंक तक, सब में इस बात पर आम सहमति है कि भारत में उपभोग असमानताएं निश्चित रूप से कम हुई हैं।
लेकिन दूसरी ओर आलोचक भारत में बढ़ती असमानताओं का तर्क आगे बढ़ा रहे हैं, वे इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ग़रीबी और उपभोग में समानताएं दोनों पहले से कम हो गए हैं।
क्या कहते हैं आलोचक?
आलोचकों का पहला तर्क यह है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें आय और संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। उपभोग आधारित गिनी सहगुणांक असमानताओं को कम करके आंकता है, क्योंकि अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। उसके मुकाबले आय आधारित समानताएं अधिक विस्तृत अवधारणा है और उस संदर्भ में भारत में आय और संपत्ति की असमानताएं वास्तव में बढ़ी है। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया गया सर्वेक्षण उपभोग को ठीक प्रकार से आकलन नहीं कर पाया। ऊपर के पांच प्रतिशत अमीर सामान्य सर्वेक्षण में अपने उपभोग को कम करके बताते हैं और उस आधार पर निष्कर्ष सही नहीं होगा।
आलोचकों का यह भी कहना है कि 2011-12 और 2022-23, जिन दो वर्षों के बीच तुलना की गई है उनकी क्रियाविधि (मेथाडोलॉजी) में काफी अंतर है इसलिए वह तुलना भी ठीक नहीं है।
आलोचकों का कहना है कि कुल 49 प्रतिशत राष्ट्रीय उपभोग को ही सर्वेक्षण में शामिल किया जा सका है, क्योंकि अमीरों द्वारा अपने उपभोग को कमतर बताया जाता है इसलिए इसके आधार पर सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी सर्वेक्षण सभी पहलुओं में परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए इन तर्कों के आधार पर हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि जब एक के बाद एक रिपोर्ट गरीबी में कमी का संकेत दे रही हैं, चाहे वह अत्यधिक गरीबी हो या बहुआयामी, उपभोग असमानताओं में कमी भी एक वास्तविकता है। भारत में वर्तमान सरकार की समावेशी नीतियों के कारण ऐसा हो सका है। पहली बार इतने कम समय में ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ घरों के निर्माण से अभावग्रस्त लोगों का जीवन बदला है। इसके साथ ही सभी घरों में बिजली, अधिकांश आबादी को पाइप से जल कनेक्शन और स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन की उपलब्धता, साथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक सीमा से कम आय वाले प्रत्येक पात्र परिवार को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को ग़रीब बनाने वाले कारकों को समाप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही, हम यह भी देखते हैं कि पहले भी सरकारें समाज के गरीब तबके के उपभोग में सुधार के नाम पर भारी धनराशि खर्च करती थीं, लेकिन खामियों के कारण भारी भ्रष्टाचार और लीकेज होता था। लेकिन शून्य बैलेंस वाले 53 करोड़ से ज़्यादा जन धन बैंक खाते खोलने और इन सभी खातों को आधार व मोबाइल नंबर से जोड़ने से, बिना किसी लीकेज के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संभव हुआ। इससे न केवल सरकार का खर्च कम हुआ, बल्कि लोगों के उपभोग मानकों में सुधार लाकर उनके जीवन में निश्चित सुधार हुआ है। इसलिए, असमानताओं का आकलन करने वाले घरेलू सर्वेक्षणों की कमियों और कमज़ोरियों को तो समझा जा सकता है, लेकिन गरीबी में निश्चित रूप से कमी आई है, चाहे वह चरम पर हो या बहुआयामी। यही बात गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) में भी दिखाई देती है, जो उपभोग असमानताओं में कमी दिखाती है। लेकिन इसे अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हालाँकि असमानताएँ कम हुई हैं, लेकिन असमानताओं में कमी का श्रेय सरकारी सहायता और कुछ हद तक मुफ्त सुविधाओं को जाता है; लेकिन हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार अनंत काल तक गरीबों और वंचितों का समर्थन करती रहेगी। दीर्घकाल में, हमें लोगों को इतना सक्षम बनाना होगा कि वे अपने परिवारों की ज़रूरतें पूरी कर सकें, जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, पानी आदि। लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना होगा और देश में विकेंद्रीकरण के आधार पर छोटे व्यवसायों और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना होगा, ताकि हम वितरण में अपेक्षित समानता के दीर्घकालीन उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।