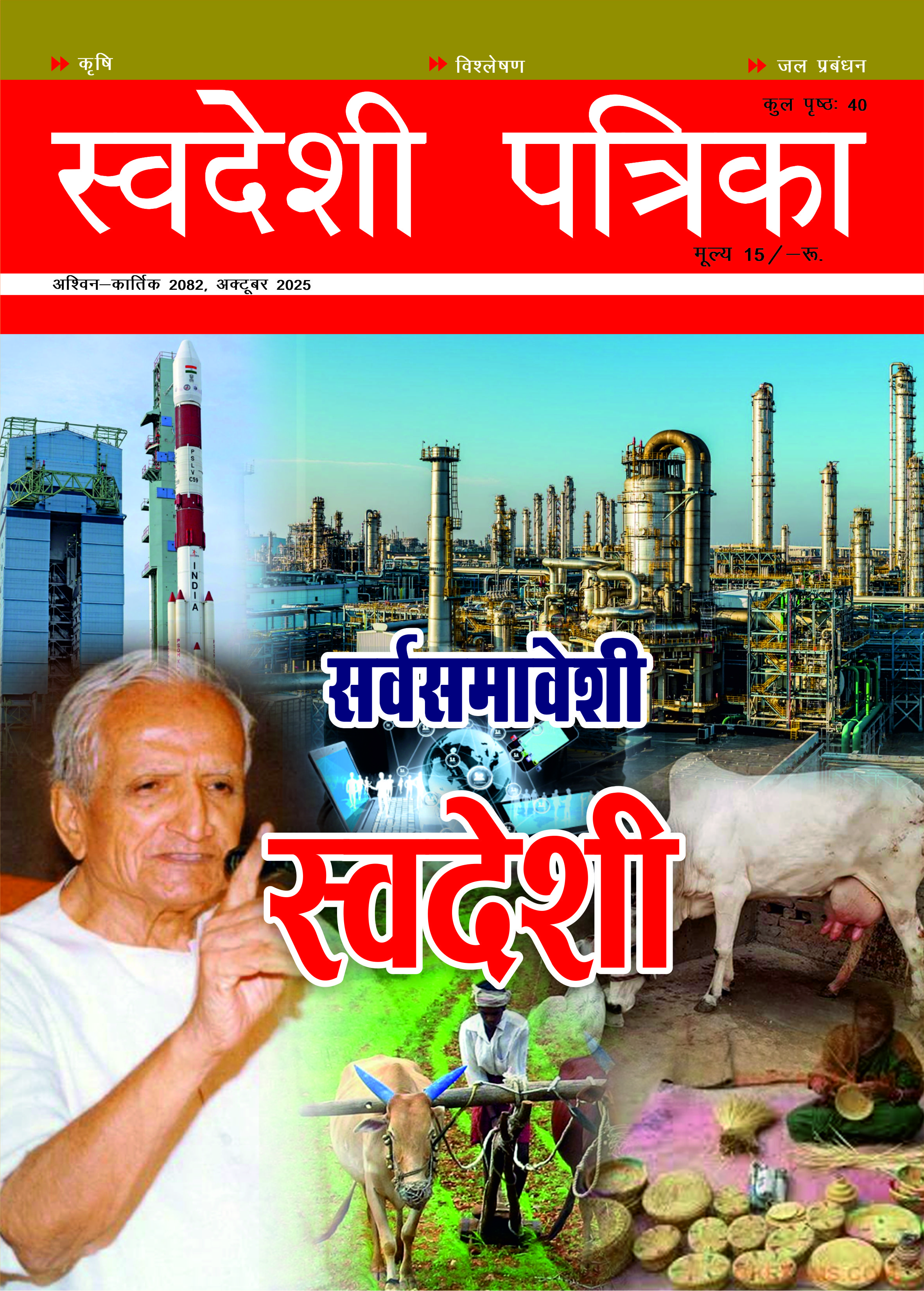मंदीः चुनौतियां और उपाय
इन दिनों विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं मंदी के अंदेशे में है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी साल 2024 कठिन और मुश्किल भरा रहा है। विकास की राह में सबसे ज्यादा अड़चन महंगाई ने पैदा की। आर्थिक विकास की कहानी में मंदी आई है, लेकिन देश की दीर्घकालीन क्षमता बरकरार है। राजकोषीय प्रोत्साहन, मौद्रिक नीति समायोजन और संरचनात्मक सुधारों के सचेत प्रयास से भारत न सिर्फ मौजूदा चुनौतियों से निपट सकता है, बल्कि अपेक्षित विकास की कहानी फिर से पटरी पर आ सकती है। - के.के श्रीवास्तव
वर्ष 2024 के प्रथम तीन तिमाहियों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जो देश की दीर्घकालीन विकास संभावनाओं के बारे में सरकार के आश्वासन के बावजूद चिंता का विषय है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत तक पहुंचाने की उम्मीद है, जो कि संभावित रूप से सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान कायम रख सकती है। हालांकि विकास की यह दर रोजगार सृजन, आय असमानता और सतत् विकास जैसी भारी दबाव वाली चुनौतियों को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की अर्थव्यवस्थाओं ने अपने उच्च विकास चरणों में लगातार 8 प्रतिशत से अधिक विकास दर हासिल किया है। विकास की ऊंची दरों के कारण वहां मजबूत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला, आय की असमानता पर बहुत हद तक काबू पाया गया और प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। भारत की मौजूदा विकास दर के साथ इन मोर्चों पर उस तरह के नतीजे देने के लिए उत्साह कम ही दिखा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यह मंदी अस्थाई अथवा चक्रीय है? या यह कोरोना महामारी के उपरांत कम आधार संसाधनों द्वारा संचालित होने के बावजूद प्राप्त सुधार के बाद महामारी पूर्व के रुझानों की वापसी के संकेत है? ऐसे में अहम बात यह है कि किसी भी रूप में मौजूदा मंदी अनुमान से कहीं अधिक गंभीर है और इस पर शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।
मंदी के मुख्य कारक
वर्तमान में निर्माण, विनिर्माण, बिजली और उपयोगिताएं जैसे द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण दबाव डाल रहे हैं। स्वस्थ कॉर्पोरेट के समृद्ध बैंकिंग तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के बावजूद निजी पूंजीगत व्यय स्थिर हो गया है। पशु आत्माओं की कमी या भविष्य में मजबूत मांग की प्रत्याशा में निवेश की इच्छा ने एक दुष्चक्र पैदा कर दिया है। निवेश करने के लिए व्यवसायों के बीच उभरी हिचकिचाहट ने उपभोक्ता मांग को कम कर दिया है, जिससे आर्थिक विकास में सीधे तौर पर बाधा आ रही है। वित्तमंत्री और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित प्रमुख नीति निर्माताओं ने उधार लेने और खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश की है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रस्ताव पर मुद्रास्फीति संबंधी चिताओं का हवाला देते हुए सदैव अपनी ओर से सावधानी बरत रहा है। यह ठीक है कि असुरक्षित गैर बैंक ऋण पर सख्त नियमों के चलते उपभोक्ता खर्च और अधिक संकुचित हुआ है। ऐसे में ब्याज दरों को कम करने से अस्थाई बढ़ावा मिल सकता है लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता की कीमत पर विकास को प्राथमिकता देना जोखिम पैदा करना है। साथ ही राजकोषीय समेकन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता विकास प्रोत्साहन के रूप में सार्वजनिक खर्च में वृद्धि की गुंजाइश को कम करती है।
धीमी वृद्धि ने दीर्घकालिक निहितार्थ
कोरोना महामारी के बाद सुधारात्मक चरण के दौरान भारत ने अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में लचीलापन दिखाया है। हालांकि देश के 150 करोड़ नागरिकों के लिए एक सभ्य जीवन मुहैया कराने हेतु 7 प्रतिशत की न्यूनतम विकास दर को बनाए रखना आवश्यक है। वर्तमान में भारत का जनसांख्यिकीय के लाभांश लगातार कम हो रहा है, क्योंकि कम उपयोग की गई युवा क्षमता और समग्र जनसंख्या में उनकी घटती हिस्सेदारी इसका प्रमुख कारण है।
हाल के दिनों में खड़े हुए भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार युद्ध के पार्श्व में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भारत की चुनौतियों को और बढ़ा रही है। वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख खिलाड़ी चीन अति क्षमता से जूझ रहा है, जबकि ट्रंप 2.0 के तहत संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की संभावित वापसी भारत के निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। घरेलू मोर्चे पर विनिर्माण वृद्धि पिछली तिमाही में तेजी से गिरते हुए 7 प्रतिशत से 2.2 प्रतिशत तक नीचे आ गई है, जो व्यापक आर्थिक कमजोरी को दिखाती है। खासकर निम्न आय समूह में शहरी खपत भी कमजोर हुई है। लगभग 6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति और स्थिर मजदूरी ने क्रय शक्ति को बिल्कुल कमजोर बना दिया है। खाद्य मुद्रा स्थिति का स्तर 10 प्रतिशत से अधिक होने से घरेलू वित्तीय तनाव बढ़े हैं, जिससे कि विवेकाधीन खर्च और खपत के स्तर में भारी कमी दर्ज की गई है। निजी खपत जुलाई-सितंबर तिमाही में सिर्फ 6 प्रतिशत रहा, जो पिछली तिमाही के 7 प्रतिशत के आंकड़े से कम है। शहरी भारतीयों का खर्च जीडीपी की वृद्धि में अहम योगदान करता है लेकिन यह तबका मुद्रास्फीति समायोजित मजदूरी में स्थिरपन या गिरावट का सामना कर रहा है। अक्टूबर 2024 के बाद से पूंजी बहिर्वाह के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। निवेशकों के विश्वास में कमी आई है। दूसरी तरफ यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा दरों को आपेक्षित रूप से कम करने में अनिच्छा प्रकट करने के कारण विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार अब कम आकर्षक बन गए हैं।
चुनौतियों के बीच उज्जवल स्थान
देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र ने जुलाई-सितंबर तिमाही में 3.5 की वृद्धि दर्ज की है। आगे भी अनुकूल मानसून की संभावना है। कृषि वृद्धि के कारण ग्रामीण मांग में तेजी आई है जो शहरी मंदी का प्रतिकार करती है। यदि लक्षित सरकारी उपायों द्वारा इसे पर्याप्त रूप से समर्थन किया जाता है तो यह ग्रामीण मांग अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ज्ञात हो कि सार्वजनिक व्यय अपने स्वस्थ गति से लगातार चल रहा है जो की आर्थिक प्रतिकूलताओं के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। 80 करोड लोगों को मुक्त राशन दिया जा रहा है।
मौद्रिक प्रोत्साहन एक ‘दो-धारी तलवार’
अभी देश में सबसे अधिक बहस मौद्रिक प्रोत्साहन को लेकर चल रही है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति संबंधी चिताओं को आगे करते हुए बेंचमार्क ब्याज दरों को 6.5 प्रतिशत से कम करने की मांग का विरोध किया है। फिर कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक माहौल में दरां में कटौती की जरूरत है। उनका तर्क है कि उच्च आधार लागत क्षमता निर्माण और नए निवेश को हतोत्साहित करते हैं, जिससे विनिर्माण और शहरी मांग में मंदी उपजती है।
हालांकि ब्याज दरों में कटौती कोई रामबाण नहीं है, लेकिन इससे वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बढ़ावा मिलता है। कम उधार लागत ऋण चुकौती के बोझ कम कर सकते हैं, जिससे खपत को बढ़ावा मिल सकता है। कम वित्तीय पोषण लागत से व्यवसाय भी लाभान्वित हो सकते हैं। संभावित रूप से निवेश गतिविधि फिर से पटरी पर आ सकती है। हालांकि मौद्रिक सहजता का प्रभाव आमतौर पर देरी से संचालित होता है जो पूरक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है।
संरचनात्मक सुधार समय की मांग
केवल मौद्रिक सहजता मंदी के मूल कारणों को संबोधित नहीं कर सकती। विनिर्माण क्षमता की अधिकता से निपटने, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और घरेलू उद्योगों को कमजोर करने वाले सस्ते आयातों की डंपिंग को रोकने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक है। सरकार को तकनीकी प्रगति को भी प्राथमिकता देनी चाहिए और वैश्विक बदलावों का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए ‘चीन प्लस वन’ रणनीति, जिसका उद्देश्य चीन से परे आपूर्ति श्रंखलाओं में विविधता लाना है। दुर्भाग्य से भारत ने इस अवसर का पूरी तरह लाभ नहीं उठाया है। आपूर्ति पक्ष के मसले महत्वपूर्ण है, जबकि मंदी का प्रमुख कारण मांग पक्ष है। इस समय खपत, निवेश तथा मांग सभी कमजोर स्थिति में है। बड़ी कंपनियों ने मुनाफे के बाद भी क्षमता विस्तार, वेतन में वृद्धि आदि को बांधकर रखा है। इसके चलते निवेश चक्र में ठहराव है तथा मांग में कमी है।
आगे का रास्ताः समन्वित नीति कार्रवाई
भारत की अर्थव्यवस्था मौलिक रूप से लचीली है, लेकिन वर्तमान मंदी के चेतावनी संकेत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए संभावित प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले मंदी से प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित सहायता प्रदान करने के लिए राजकोषीय नीति का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना मांग को उत्तेजित करने का रास्ता तैयार हो सके।
दूसरा, मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यदि मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम हो जाता है तो रिजर्व बैंक उधार लेने और निवेश का समर्थन करने के लिए ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है।
तीसरा, दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधारों को तेज किया जा सकता है। श्रम उत्पादकता में सुधार बुनियादी ढांचों को बढ़ाने और नियामक ढांचे को सरल बनाने के उद्देश्य से नीतियां निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकती है। और अंत में निर्यात संवर्धन पर मुख्य ध्यान होना चाहिए। व्यापार साझेदारी को मजबूत करना, निर्यात में विविधता लाना, वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्थात्मकता को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। वर्तमान मंदी से उबरने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण जरूरी है। इसके लिए समावेशी और सतत विकास का नजरिया जरूरी ह,ै जो लोगों की जरूरत को प्राथमिकता देता हो।
मोटे तौर पर मंदी चिंताजनक तो है, लेकिन यह विकास के कारकों पर पुनर्विचार करने और उन्हें पुनः संतुलित करने का अवसर भी प्रस्तुत करती है। नवाचार, समन्वित नीतिगत कार्रवाई और संरचनात्मक सुधारों के जरिए भारत अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा अधिक मजबूती से आगे बढ़ सकता है।
निष्कर्ष
भारत की आर्थिकी सदैव लचीली रही है। फिर भी मंदी की चुनौतियां विकट है लेकिन इस आपदा में अवसर भी है। भारत अपनी कमजोरी को दूर करते हुए अंतर्निहित शक्तियों को दोहन कर न केवल मंदी से उबर सकता है बल्कि भविष्य में उच्च विकास का मॉडल भी पेश कर सकता है। ध्यान रहे विकास का अर्थ सिर्फ जीडीपी संख्या हासिल करना नहीं है, यह राष्ट्र की समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने से संबंधित है। यह समय उठ खड़े होने और उचति कार्रवाई करने का है। सकारात्मक बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2026 में देश की जीडीपी 7 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि मानसून एक बार और सामान्य रहने वाला है।