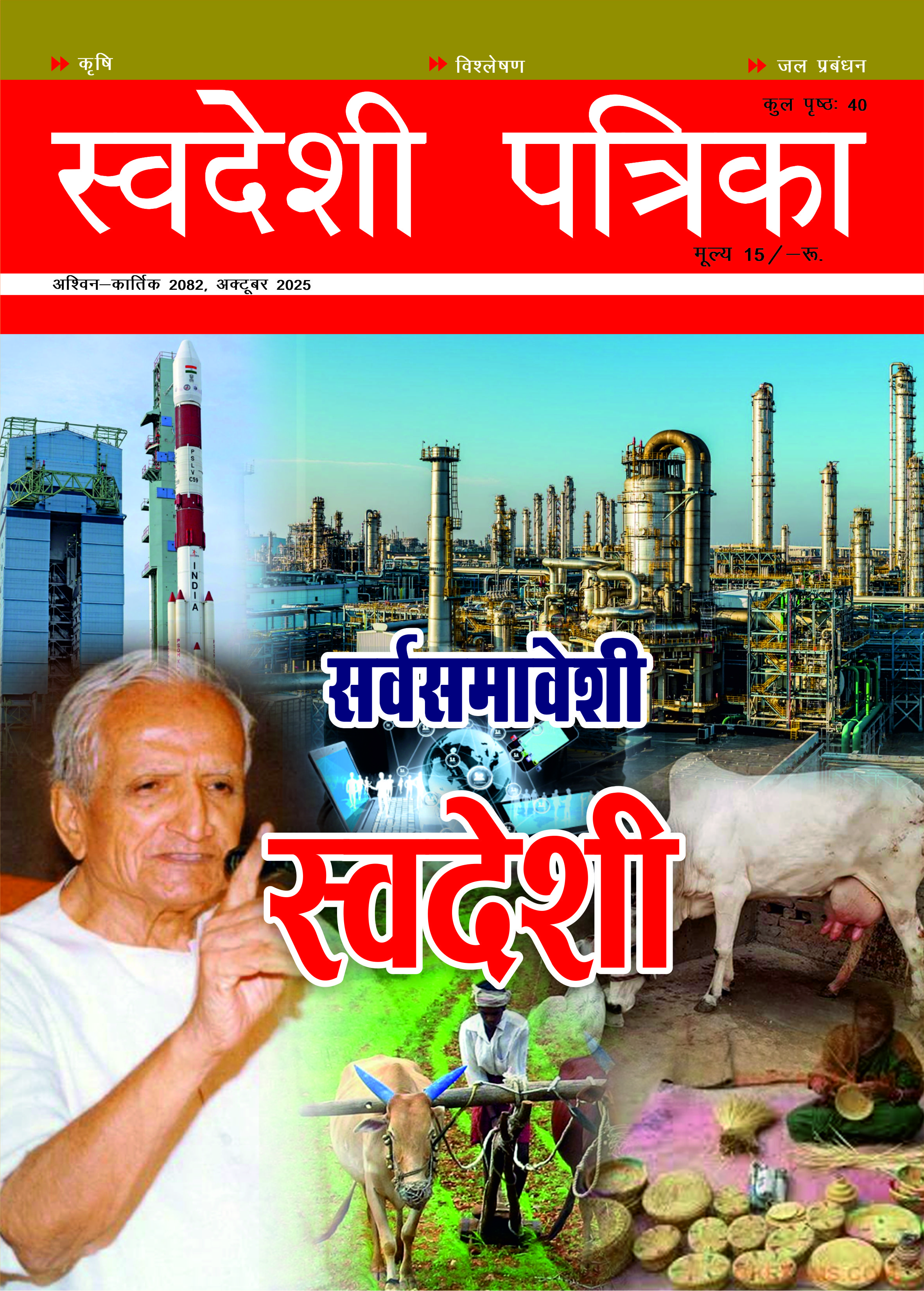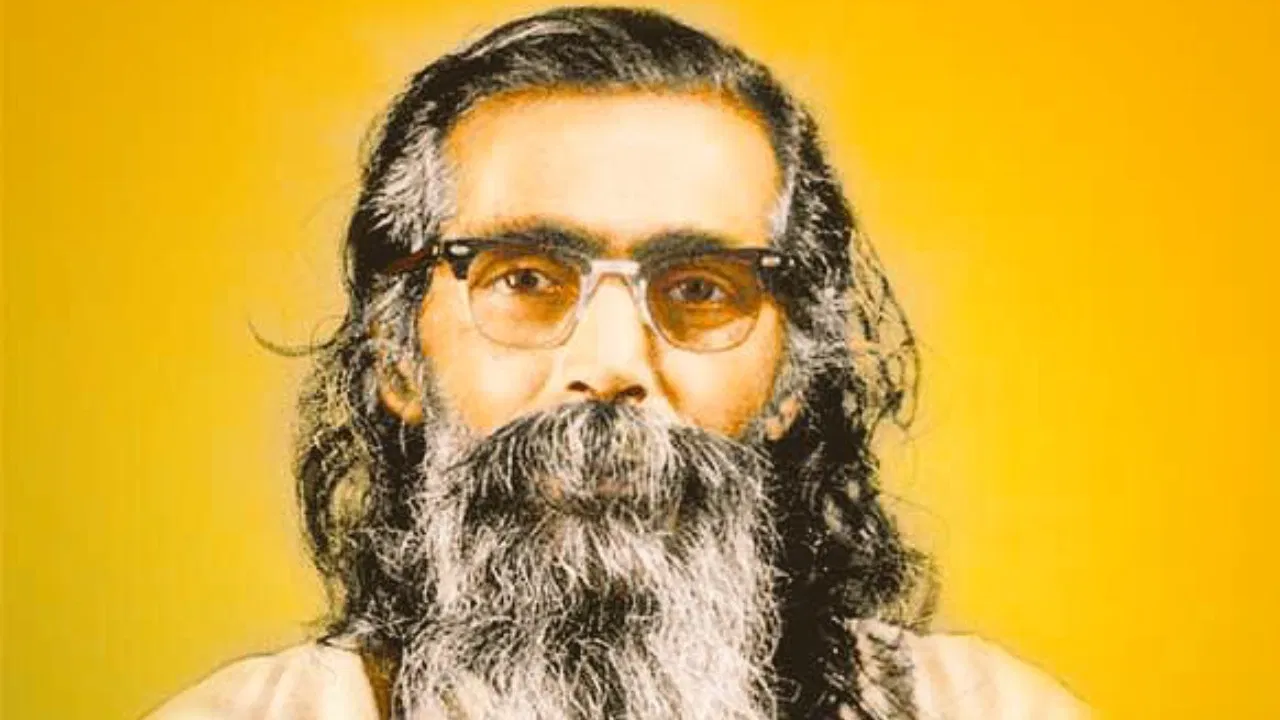
विकास हेतु स्वदेशी को जरूरी मानते थे श्री गुरूजी
— Swadeshi Samvad
दिनांक 9-10 सितम्बर, 1952 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा में स्वदेशी पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। श्री गुरूजी से यह पूछा गया कि विदेशी सत्ता की समाप्ति के 5 वर्ष पश्चात इस प्रस्ताव का क्या औचित्य है। श्री गुरूजी ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी विरोध की भावना के कारण लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति सहज आकर्षण था। कांग्रेस द्वारा श्री गाँधीजी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। लोकमान्य तिलक युग में निर्मित स्वतंत्रता आंदोलन की चतुर्सूची योजना का स्वदेशी एक प्रमुख मुद्दा था। डॉ. हेडगेवार ने तो स्वदेशी चेतना को ही संघ के आचार तथा विचारों का अधिष्ठान बनाया था। लेकिन आजादी के पश्चात देश में विदेशी वस्तुओं का अधिक प्रयोग होने लगा है। अतः प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्ताव में स्वयंसेवकों से यह आग्रह किया गया था कि पहले वे स्वयं स्वदेशी का दृढ़ व्रत लें और बाद में लोगों को इस दिशा में प्रवृत करें। इस दृष्टि से वर्धा के डॉ. कुमारप्पा को दिनांक 25 सितम्बर, 1952 को श्री गुरूजी ने अपने पत्र में लिखा ’स्वदेशी के विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रथम स्वराज प्राप्ति का शस्त्र और तदनंतर उसको सुरक्षित एवं उन्नत रखने का आधार स्वदेशी ही है। हम लोगों ने अपने संघ के कार्य द्वारा इस व्रत के आचरण का आग्रह अधिक तीव्रता से प्रसारित करने का निश्चिय किया है।“
स्वदेशी जीवन पद्धति
व्यक्तिगत जीवन में छोटी बातों में भी स्वदेशी जीवन पद्धति का श्री गुरूजी का आग्रह रहता था। यदि गलती से हाथ धोने के लिए उन्हें विदेशी साबुन दे दिया जाता तो राख से हाथ साफ कर वे धीरे से कह देते थे कि विदेशी साबुन से राख मली।
स्वभाषा प्रेम
आंग्ल भाषा के विद्वान होने के बावजूद भी विवाह का निमंत्रण, कार्यक्रम पत्रिका, अभिनंदन संदेश आंग्ल भाषा में छापना भी गुरूजी को अच्छा नहीं लगता था। पुणे के न्याय रत्न धुंडिराज शास्त्री को दिनांक 13-7-55 के पत्र में वे लिखते हैं यज्ञ करने के विषय में आपका पत्रक योग्य समय पर प्राप्त हुआ परन्तु यह अंग्रेजी में लिखा हुआ देखकर विचित्र सा लगा। यज्ञ जैसे पवित्र समारोह का व्यवहार अनार्य में भाषा हो, यह मेरे मन को अच्छा नहीं लगा। इसलिए इस विषय में अत्यन्त आदर और उत्सुकता होकर भी इस समय मुझे लगता है कि इस उपक्रम से संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए क्षमा करें। इसके विपरीत मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पण्डित रवि शंकर शुक्ल द्वारा शासन कार्यहेतु प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार करने पर उनका अभिनंदन करते हुए दिनांक 2-9-1953 को गुरूजी ने अपने पत्र में लिखा “आज से विधिवत आपने मध्य प्रदेश, राज्यशासन में विदेशी भाषा अंग्रेजी को दूर कर हिन्दी तथा मराठी भाषाओं का व्यवहार आपने प्रारम्भ कर दिया, यह जानकर अतीव प्रसन्नता एवं समाधान का अनुभव कर रहा हूँ, इस उत्कृष्ठ निर्णय को प्रत्यक्ष में लाने में अनेक कठिनाइयां होते हुए भी राष्ट्राभिमान के संतोष के निर्मित उन्हें झेलकर पार करने की दृढता आपने प्रकट की है। इस महान कार्य के लिए मैं अपनी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से आपका एवं आपके शासकीय सहकर्मियों का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूँ।“
श्री रजनीकांत मुद्गल ने श्री गुरूजी के हस्ताक्षर मांगते हुए एक पत्र लिखा। उसके उत्तर में उन्होंने लिखा मेरे इस पत्र से आपकी हस्ताक्षर की मांग तो पूर्ण हो जायेगी किन्तु हस्ताक्षर मांगने का आपका यह अंग्रेजी ढंग का उद्योग मुझे उचित नहीं लगता। किसी की स्वाक्षरी या हस्ताक्षर पास रखने से यदि इस व्यक्ति के संबंध में मन में सद्भावना उत्पन्न होती हो, तो उसके तत्त्व तथा गुण अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना उचित है।
स्वदेशी वेश भूषा
श्री गुरूजी स्वदेशी वेश भूषा के न केवल समर्थक थे बल्कि इसका आग्रह भी करते थे। उनका मानना था कि यदि हम अपनी पद्धतियों का अवलम्बन करें तो विदेशियों तक में हमारे बारे में सम्मान की भावना निर्मित होती है। इस संबंध में वे अपना स्वयं का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, मैं नागपुर में स्कारिश मिशनरियों द्वारा संचालित एक महाविद्यालय में पढ़ता था। एक बार हम विद्यार्थियों ने पूर्णतः महाराष्ट्रीय पद्धति के भोजन का कार्यक्रम निश्चित किया। इसके लिए प्राचार्य एवं दो यूरोपीय प्राध्यापकों को निमंत्रित किया गया और उन्हें बताया गया कि भोजन धोती पहन कर उधाडे बदन (कपड़े निकालकर) पीढ़े पर बैठकर करना होगा। प्राचार्य के लिए ईसायत का अहंकार आड़े आ गया और उन्होंने हमारा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। परन्तु दो वयोवृद्ध प्राध्यापकों ने निमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने ही प्राचार्य को भी तैयार कर लिया। इन तीन यूरोपियों ने धोती पहन कर उघाड़े बदन महाराष्ट्रीय पद्धति से हम लोगों के समान ही हाथों का उपयोग करते हुए भोजन किया। इसी विषय पर श्री गुरूजी ने कहा कि ईश्वर चन्द्र विद्या सागर ने वायसराय कार्यकारी मण्डल की बैठक में जाते समय अंग्रेजी वेशभूषा न पहनने का निश्चिय किया। बंगाली ढंग के वस्त्र पहनकर ही वे उपस्थित हुए और उन्हीं को ’कार्यकारी मण्डल की बैठक में सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुआ। उनका स्वागत करने और विदा करने हेतु स्वयं वायसराय मंच से उतर कर आये।
मन में रमे स्वदेशी
श्री गुरुजी यह सोचते थे कि जीवन के अंग-प्रत्यंग में स्वदेशी भावना का प्रकटीकरण हो। अंग्रेजी तिथि तथा सन के स्थान पर भारतीय तिथि तथा संवत व पाश्चात्य पद्धति के 24 घंटे के दिन के स्थान पर भारतीय पद्धति के 60 घटिकाओं के प्रचलन को वे स्वदेशीकरण का आवश्यक अंग मानते थे। कुछ घड़ी निर्माताओं के समक्ष इसी प्रकार के घड़ी के निर्माण का विचार भी उन्होंने प्रकट किया था।
मानववाद ही सर्वश्रेष्ठ
श्री गुरूजी समाजवाद, पूँजीवाद की अपेक्षा आर्थिक क्षेत्र में मानववादी थे. समाजवाद एवं पूँजीवाद ने मनुष्य को व्यवस्था के - निर्जीव यंत्र का एक पुर्जा मात्र बना दिया। हमें सम्पूर्ण मनुष्य का विचार करना होगा, जिसके पास हृदय, मस्तिष्क और शरीर तीनों की भूख है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाने के कारण सुख के स्थान पर दुख आता चला जायेगा।
गोमाता के प्रति श्रद्धा
गो हत्या निषेध संबंधी एक सभा में गुरूजी ने कहा जिस राष्ट्र का श्रद्धास्थान नष्ट हो जाता है, उस राष्ट्र के अभ्युदय की कामना करना व्यर्थ है। अब हमें यह सोचना है कि सर्व मान्य श्रद्धा केन्द्र कौन सा है? राष्ट्र में राजनीतिक या पंथिक भिन्नता भले ही हो, एक निर्विवाद सत्य है कि गो वंश का नाम लेते ही श्रद्धा की भावना जागृत होती है। अपने हृदय में गोमाता के प्रति श्रद्धागान बजायें। अपने अंतःकरण तथा राष्ट्रजीवन में पराकोटि का तेजस्विता निर्माण करें। इसी संबंध में वे आगे कहते हैं मैं समझता हूँ कि श्रद्धा के विषय में आर्थिक मापदण्ड लगाना अनुचित है। उदाहरण के लिए अपने राष्ट्र का ध्वज है उसे उतारकर तोड़ फोड़ दें तो कौन सी बड़ी हानि हो गयी। लेकिन इन की रक्षा के लिए कितना भी धन जन का मूल्य क्यों न देना पड़े, सर्वथा रक्षणीय है।
उद्योगों का विकेन्द्रीकरण
श्री गुरूजी चाहते थे कि देश में लघु एवं गृह उद्योगों का जाल फैले। वे बड़े औद्योगिक केन्द्रों का पोषण करें जैसे परिदृश्य जापान में हैं। उन्होंने 1949 में ही चेताया था कि इन दिनों औद्योगिकीकरण किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मापदंड बन जाने के कारण विश्व संघर्ष तथा युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। सच्चे प्रजातंत्र का आधार आर्थिक विकेन्द्रीकरण ही हो सकता है। अतः हमें छोटे-छोटे उद्योगों को ही अपनाना चाहिए। एक संदर्भ में श्री गुरुजी कहते हैं, युद्ध के बाद जापान और पश्चिमी जर्मनी उस समग्र आर्थिक रूपांतरण के जादू के जीवंत प्रमाण है, जो वहां के नागरिकों के अनुशासित प्रयासों व राष्ट्रभक्ति के उत्साह का परिणाम है। प्रत्येक जापानी के हृदय की धड़कन से एक ही आवाज आती है - ‘देश प्रथम’।
ग्रामों की आत्मनिर्भरता
वर्ष 1952 में एक कार्यक्रम में श्री गुरूजी शिवणे ग्राम गये। वहां ग्रामीणों ने मिलकर 1200 फुट लम्बा एक रास्ता तैयार किया था। वहां अपने भाषण में उन्होंने कहा ग्रामीणों ने अपने परिश्रम और स्वावलम्बन से गाँव की एकता की सामर्थ्य से यहां रास्ता बनाकर एक कदम आगे बढ़ाया है। विदेशों से आने वाली सहायता अथवा यंत्रों पर निर्भर रहकर हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, लेकिन क्या गाँव के ही लोग स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों और अपने गाँव की उन्नति के लिए यतन करें, यह श्रेष्ठ नहीं है। गाँधी जी कहा करते थे कि मैं विशाल उत्पादन चाहता हूँ परन्तु विशाल जन समूह के द्वारा उत्पादन चाहता हूँ। आज जब वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण के नाम पर देश को विदेशियों के हवाले किया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में परम पूज्य श्री गुरूजी के स्वदेशी संबंधी विचारों को व्यवहार में लाने की ज्यादा आवश्यकता है। स्वदेशी राष्ट्र भक्ति का एक सशक्त माध्यम है। व्यक्तिगत जीवन, समाज जीवन एवं राष्ट्रजीवन में स्वदेशी का भाव एवं व्यवहार बढ़े, ऐसा आग्रह है।
(स्वदेशी पत्रिका से साभार)