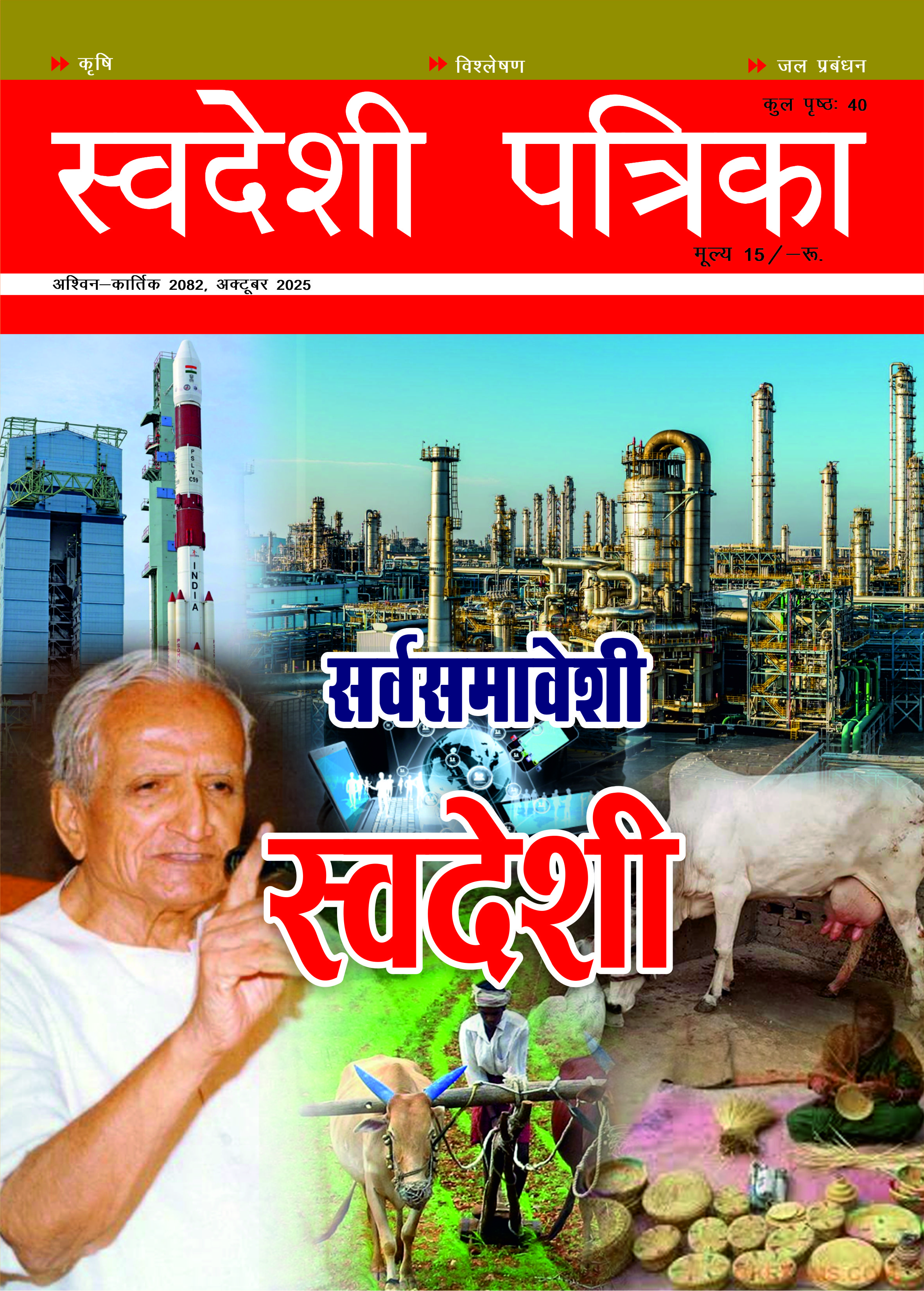असत्य एवं अविवेक पर आधारित ट्रंप की भ्रामक टैरिफ नीति
भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के कमजोर पक्षों को सुधारने और भविष्य के मार्ग पर विचार करने की आवश्यकता है। - विनोद जौहरी
वर्तमान में विश्व भर से अमेरिकी टैरिफ नीति पर तीखी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीति केवल उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षा और अमेरिका फ़र्स्ट के उनके ध्येय के लिए समकक्षी अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करना है। निश्चित रूप से भारत उनका लक्ष्य है। जिस दुराग्रह से उन्होने ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया है उससे तो कोई संदेह नहीं रह जाता कि उनकी भारत के प्रति टैरिफ नीति का दोनों देशों के व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। वैश्विक परिपेक्ष्य में भी यही दृश्य परिलक्षित होता है। यह सही हैं कि भारतीय प्रतिनिधि मण्डल अभी भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता में हैं, जिसका परिणाम अभी समझना कठिन है। अपने दूसरे कार्यकाल के प्रारंभ से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विभिन्न देशों के साथ भारी टैरिफ ड्यूटी लगाने के निर्णय से वैश्विक व्यापार में बढ़े स्तर पर भूकंप खड़ा कर दिया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ नीति का विरोध हो रहा है और इसके संवैधानिक औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लग गये हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त हुए आठ दशक बीत गये हैं परंतु विश्व की महाशक्तियों को अभी यह समझ नहीं आया है कि उनके वर्चस्व के पराभव का समय आ चुका है। इनके वर्चस्व का सबसे बड़ा हथियार संयुक्त राष्ट्र संघ है और जिसका सबसे पहला शिकार भारत ही है जिसके संरक्षण और प्रभाव से भारत का विभाजन हुआ और आज तक न केवल भारत उसके परिणाम भुगत रहा है बल्कि विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान और वर्तमान बंगलादेश पूरी तरह बर्बाद हुए हैं जिनकी कुल बयालीस करोड़ जनता लगातार धार्मिक उन्माद, गृह युद्ध जैसी स्थिति, अशांति और आर्थिक कंगाली झेल रही है। विश्व की महाशक्तियों ने दुनिया को कितने ही युद्धों में धकेला है और तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर रखा है। इसके अलावा अफ्रीका में भुखमरी और विश्व में महामारियों के समय इन महाशक्तियों का असंवेदनशील चरित्र उजागर हुआ है जिसका सबसे नया उदाहरण कोरोना महामारी है। पिछले आठ दशकों में इन महाशक्तियों विशेष कर अमेरिका का सबसे अधिक हस्तक्षेप का क्षेत्र पश्चिम और मध्य पूर्व एशिया है जहां युद्ध की ज्वाला और ज्वालामुखी धधकते रहते हैं। विश्व में इस विनाशलीला को विश्व की महाशक्तियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर तमाशा देखती रहती हैं। विनाश की इस परिक्रमा में वैश्विक व्यापार तो बहुत छोटा सा पक्ष रह जाता है, उसमें भी अमेरिका और चीन की वर्चस्ववादी एवं संरक्षणवादी नीतियां और विश्व व्यापार संगठन की विवशता और उसके इन महाशक्तियों को समर्थन देना विकासशील देशों के प्रति दुराग्रह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक भी इन्हीं महाशक्तियों की कठपुतलियाँ हैं और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान जैसे देशों को पुरस्कार के रूप में अनुदान देती हैं। यदि स्पष्टता से स्वीकार करें तो इन महाशक्तियों की समृद्धि दूसरे देशों के आर्थिक शोषण से है।
टैरिफ के चलते छंटनी की संभावनाओं के संदर्भ में अपने अंतिम कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर पच्चीस प्रतिशत टैरिफ और रूस से पैट्रोलियम खरीदने पर भारी जुर्माने के समाचार से अमेरिका के एक सुपर पावर होने योग्य व्यवहार को नहीं दर्शाता है। भारत को अमेरिका से रक्षा और शोध, टैक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में व्यापार पर प्रभाव पड़ना तय है। इस बीच पाकिस्तान में कच्चे तेल के भंडार और उत्पादन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प ने जो नया विमर्श खड़ा किया है उसका लाभ सीपैक के कारण चीन को है, अमेरिका को तो किसी भी दृष्टि से लाभ की संभावना नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तानी तेल को लेकर भारत, तेल उत्पादक देशों और चीन पर एक साथ लक्ष्य साधने का जो प्रयास किया है, वह निष्फल है। अमेरिका ने यह देख और समझ लिया है कि भारत झुकने वाला देश नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। टैरिफ पर भारत की सधी हुई प्रतिक्रिया प्रशंसनीय है।
भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहकर उन्होंने देश का घोर अपमान किया है और यह भारत के आत्म सम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है। हम अमेरिका के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मित्र रूस को नहीं छोड़ सकते। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को अपने रास्ते बदलने होंगे और यह प्रतिस्पर्धा दीर्घकालिक है। भारत ने प्रारम्भ से ही स्पष्ट कर दिया है कि हम अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में आने की अनुमति नहीं दे सकते और अपने किसानों को किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं होने देंगे। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने छोटे और माध्यम औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) को भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारे उद्योग व्यापार की आधे से अधिक भागीदारी एम एस एम ई क्षेत्र की है।
जिस रूस से पैट्रोलियम खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लिया है, उसी रूस से अमेरिका 5.2 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प को यह समझना होगा कि अमेरिका की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मेरुदंड विदेशों से विदेशी व्यापार, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रायल्टी, लाइसेंस, विदेशी नागरिकों के पर्यटन, विदेशी विद्यार्थियों की फीस, वीजा से आय पर निर्भर है। जिन एशियाई देशों से ट्रंप टैरिफ नीति के बल पर आक्रामकता दिखा रहे हैं, उन सभी देशों भारत, रूस, चीन, जापान और दक्षिण एशियाई देशों सहित एशियाई देशों की कुल जीडीपी 41 ट्रिलियन डॉलर है जो अमेरिका की 30 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है।
आंकड़ों की दृष्टि से भारत अमेरिकी व्यापार को देखें तो अमेरिका का भारत से आयात 87.3 बिलियन डॉलर है जो कुल अमेरिकी आयात 3.17 ट्रिलियन डालर का मात्र 2.75 प्रतिशत है। अमेरिका का भारत को निर्यात 41.4 बिलियन डॉलर है जो कुल अमेरिकी निर्यात 3.052 ट्रिलियन डॉलर का मात्र 1.34 प्रतिशत है।
अमेरिका का कुल व्यापार घाटा 1.1 ट्रिलियन डॉलर है जबकि भारत के साथ कुल व्यापार घाटा 45.7 बिलियन डॉलर के समतुल्य 4.1 प्रतिशत है। केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत द्वारा अमेरिका को 87.3 बिलियन डॉलर के निर्यात और अमेरिका से भारत द्वारा 45 बिलियन डॉलर के आयात से इतर अमेरिका को यह भी समझना होगा कि भारतीय विद्यार्थियों से अमेरिका को 8 बिलियन डॉलर की आय होती है। अकेला कोका-कोला भारत में 290 मिलियन डॉलर का व्यापार करता है। अमेरिकी इंवेस्टमेंट कंपनियां भारत में 40 बिलियन डॉलर का व्यापार करती हैं। अकेले अमेज़न जैसी विशालकाय ई कामर्स कंपनी भारत में 13 बिलियन डॉलर का व्यापार करती है। इस प्रकार भारत के साथ अमेरिका का लाभ का व्यापार है। भारत के साथ अमेरिका ने अपमानजनक व्यवहार करके आपसी संबंधों में गहरी दरार डाली है जो उसके एशिया में राजनयिक एवं सामरिक प्रभाव को क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए अमेरिका - भारत व्यापार में व्यापार घाटा भारत के लिए है और अमेरिका के लिए सरप्लस है। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया भर को भ्रमित किये हुए हैं।
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए स्वदेशी के मंत्र ही एकमात्र सफलता का सूत्र है। चीनी उत्पादों के अब भी घरेलू बाजार में बिकने का कारण यही है कि हमारे देश में दिन प्रतिदिन के सामान बनाने वाले उपक्रम बहुत छोटे स्तर पर हैं जिनको माइक्रो स्तर की औद्योगिक इकाई समझ सकते हैं जिनका उत्पादन बहुत सीमित क्षेत्र में आपूर्ति होती है या रेहड़ी पटरी पर बिकने वाले उत्पाद होते हैं। बहुत सीमित पूंजी,पुराने और लोकल मशीन, परिवार तक सीमित रोजगार देने वाले उपक्रम कभी भी चीन के सस्ते और नये उत्पादों का सामना नहीं कर सकते। फर्नीचर के मामले में भी बहुत छोटे व्यापार हैं जो केवल अपने बाजार तक ही आपूर्ति करने में सक्षम हैं। यह तो सही है कि इसलिए बहुत आवश्यक है कि घरेलू आवश्यकता की वस्तुएं विशाल स्तर पर भी निर्मित हों जो संपूर्ण देश में आपूर्ति शृंखला को पोषित कर सकें और कीमतों में भी विदेशी उत्पादों को प्रतिस्पर्धा दे सकें। इससे आगे भी सोचने की आवश्यकता है कि अब भारतीय मूल आधिक्य देशों में भी हमारे कारपोरेट हमारे स्वदेशी उत्पादों के उत्पादन के लिए स्थानीय उद्योगपतियों के साथ साझीदारी में उद्योग स्थापित करें जिससे भारतीय उत्पादों का विदेशों में, विशेषकर भारतीय मूल के करोड़ों विदेशी नागरिक उपयोग करें। भारतीय उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जाये। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के कमजोर पक्षों को सुधारने और भविष्य के मार्ग पर विचार करने की आवश्यकता है।