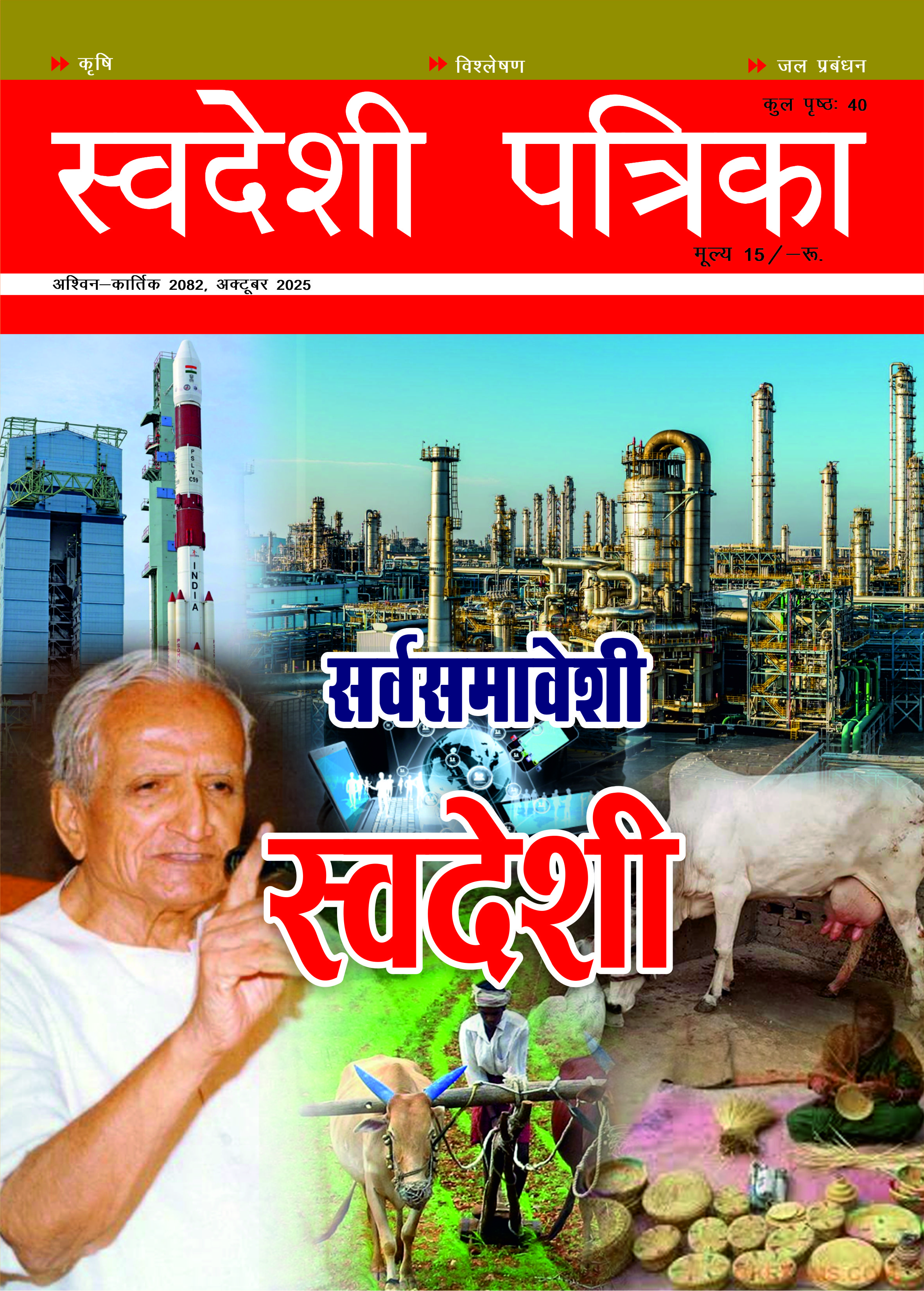ग्राम स्वास्थ्य सेवाएं समग्र बनें
ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं को सब तक सामुदायिक सहयोग से पहुंचाने का उद्देश्य सदा हमारी प्राथमिकता रहा है, पर ये सेवाएं कितने समग्र रूम में आगे जा सकेंगी, यह बहस का मुद्दा बनता रहा है। - डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के साथ-साथ ‘सबका स्वास्थ्य’ के मुद्दे पर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आरोग्य जीवन के लक्ष्य को हासिल करने हेतु गरीबों एवं बुजुर्गों को ‘आयुष्मान’ के तहत लाया गया है। ‘आयुष्मान’ कार्ड धारक देश के किसी भी अस्पताल में पांच लाख रूपये तक का ईलाज करा सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में एम्स जैसे अस्पतालों की स्थापना के सथ-साथ सरकार ने स्वस्थ भारत मिशन के तहत अपना बजटीय प्रावधान का आकार भी बड़ा किया है। सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान रूप से पहुंचाई जा सके।
ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं को सब तक सामुदायिक सहयोग से पहुंचाने का उद्देश्य सदा हमारी प्राथमिकता रहा है, पर ये सेवाएं कितने समग्र रूम में आगे जा सकेंगी, यह बहस का मुद्दा बनता रहा है। पहले सभी स्वास्थ्य समस्याओं के समग्र रूम में समाधान पर अधिक जोर दिया गया पर अनेक विकासशील देशों ने जब इसे व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के कारण उन्हें लगा कि कुछ प्राथमिकताओं को चुनकर उन्हें अधिक महत्त्व देना होगा।
इस स्थिति में ऐसे रोगों या स्वास्थ्य समस्याओं को चुना गया जिनमें कमी लाकर अधिक जीवन बचाए जा सकते थे। ऐसी प्राथमिकताओं का औचित्य समझते हुए भी अनेक स्वास्थ्यविद् ने स्वास्थ्य और विशेषकर ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी एक समग्र सोच विकसित करने की जरूरत पर ध्यान दिलाना जारी रखा क्योंकि सही अर्थों में और टिकाऊ तौर पर स्वास्थ्य सुधार इस समग्र सोच से ही संभव है। ऐसी समग्र सोच में जहां सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समावेश होता है, वहां स्वास्थ्य को नजदीकी तौर पर स्वच्छता और पोषण से जोड़ कर भी देखा जाता है। स्थानीय स्थितियों के अनुसार बेहतर पोषण के सुझाव देना तो अपेक्षाकृत सरल कार्य है, पर कठिनाई वहां आती है, जहां स्थानीय समुदायों के अनेक परिवारों (जैसे भूमिहीन और सबसे निर्धन परिवारों) में उस पोषण को प्राप्त करने की आर्थिक क्षमता ही नहीं होती है। इस स्थिति में अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने न्यायसंगत व्यापक मांग भी उठाई हैं। फिलहाल, इतना प्रयास तो वे कर ही सकते हैं कि इन परिवारों के आजीविका सुधार के कुछ व्यापक प्रयासों से जुड़ें। इसमें भी अधिक सुगम प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि सब्जी का छोटा सा बगीचा लगा कर या मुर्गी पालन से पोषण को कुछ बेहतर कर लिया जाए। इससे कुछ सुधार तो अवश्य होता है पर यदि अन्य प्रतिकूल स्थितियों से आजीविका बिगड़ रही है, तो फिर कुल मिला कर स्थिति विकट ही बनी रहती है।
अतः स्वास्थ्य कार्यक्रम में समग्रता पर जोर देने की आवश्यकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आजीविका सुधार के प्रति भी समग्र दृष्टिकोण ही अपनाया जाए। दूसरी ओर, कुछ अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इस तरह तो जिम्मेदारी और कार्य बहुत बढ़ जाएंगे। यहां एक समाधान यह हो सकता है कि यदि स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत सी आजीविका जिम्मेदारियों को संभाल न भी सकें तो कम से कम इस बारे में स्पष्ट सोच अवश्य बना लें कि आजीविका सुधार की किस दिशा में जाना है, और किन गलतियों से बचना है।
भारतीय ग्रामीण स्थिति को देखें तो प्रायः अनेक स्थानों पर छोटे किसानों और भूमिहीनों से न्याय, प्राकृतिक खेती, जल और मिट्टी संरक्षण, गांववासियों में बढ़ते सहयोग, वनों की रक्षा और स्थानीय प्रजाति के वृक्षों में वृद्धि, जैव-विविधता और परंपरागत बीजों की रक्षा, रचनात्मक रोजगार सृजन और गांव समुदाय की बढ़ती आत्मनिर्भरता का मॉडल अनुकूल और प्रेरक है। यह सोच बहुत कुछ स्वतंत्रता आंदोलन और विशेषकर महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की सोच के अनुकूल है। इस सोच पर आगे बढ़ने में कोई महंगा खर्च नहीं है अपितु किसानों के खर्च और कर्ज कम होंगे। इसके अतिरिक्त यह सोच पर्यावरण की रक्षा और टिकाऊ विकास के लिए बहुत भी अनुकूल है। इन दिनों जलवायु बदलाव के खतरे को कम करने और उसका सामना करने की क्षमता को बढ़ाने (मिटीगेशन और एडॉप्टेशन) की अधिक चर्चा है और इसके लिए धन और बजट भी उपलब्ध है। यह सोच इस दृष्टि से भी बहुत अनुकूल है और इसे अपना कर जलवायु बदलाव के खतरे को कम करने और इसका सामना करने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी बढ़ा जा सकता है।
समाज-सुधार के अनेक महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। इनमें स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि निरंतरता से शराब, तंबाकू, गुटके, ड्रग्स, गांजा आदि के विरुद्ध जन-अभियान चला कर इनका उपयोग कम से कम किया जाए। इसके लिए सभी गांवों में महिलाओं के नेतृव में नशा-विरोधी समिति बनानी चाहिए और इसका कार्य निरंतरता से चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त समग्र स्वास्थ्य के लिए समाज-सुधार के अनेक अन्य पक्ष भी महत्त्वपूर्ण हैं जैसे गांववासियों का आपसी सहयोग बढ़ना, महिलाओं की समानता और ग्रामीण कार्यों में अधिक जिम्मेदारी, बाल विवाह को रोकना, शिक्षा विशेषकर लड़कियों की शिक्षा में सुधार, जुए और अन्य कुरीतियों पर रोक। ये विभिन्न समाज-सुधार अपने आप में बहुत सार्थक हैं पर साथ ही समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने के उद्देश्य में भी इनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त यदि गांव में अहिंसा और अमन-शांति की सोच को प्रतिष्ठित और मजबूत किया जाए तो इससे भी समग्र स्वास्थ्य प्राप्ति में मूल्यवान योगदान मिल सकता है, और विशेषकर बढ़ते मानसिक तनाव और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में बहुत कमी आ सकती है। हालांकि अमन-शांति पर अधिक चर्चा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में होती है, पर हकीकत तो यह है कि दैनिक जीवन में जो हिंसा है या हिंसक सोच है, वह अनेकानेक समस्याओं और दुख-दर्द के मूल में है। वैसे तो स्थितियों में बहुत भिन्नता हो सकती है, पर अनेक गांवों में इनमें से अनेक स्थितियां महत्त्वपूर्ण स्तर पर मौजूद हैं-महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा, बहुत समय से चल रहे झगड़े और मुकदमेबाजी, जाति और धर्म आधारित भेदभाव और हिंसा, भूमि-विवाद, तरह-तरह का शोषण और उससे जुड़ी हिंसा, गुटबाजी और लठैतबाजी, हथियारों की बढ़ती उपस्थिति और अपराधी गतिविधियों की वृद्धि, संसाधनों की नियोजित लूट और इसके लिए हिंसा का उपयोग।
ये सभी प्रवृत्तियां जहां अपने आप में हानिकारक हैं, इनके कारण मानसिक तनाव, अवसाद और निराशा, बुनियादी जरूरतों से वंचित होना, भूख और कुपोषण, नशे का प्रचलन आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर, यदि दैनिक जीवन में न्याय आधारित अमन-शांति और अहिंसा स्थापित करने और आधिपत्य की प्रवृत्ति को दूर करने के प्रयास किए जाएं तो समग्र स्वास्थ्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता मिल सकती है। घरेलू हिंसा को न्यूनतम कर पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। समग्र स्वास्थ्य की यह व्यापक सोच ग्रामीण संदर्भ में विशेष तौर पर महत्त्वपूर्ण है। एक उदाहरण है, इस सोच को अपनाते हुए न केवल पोषण की मात्रा बढ़ाई जा सकती है अपितु यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्राकृतिक खेती से प्राप्त विभिन्न खाद्यों की स्वास्थ्य की दृष्टि से गुणवत्ता कहीं बेहतर होगी। दूसरी ओर, इस समग्र सोच के अनेक पक्ष ऐसे हैं, जो ग्रामीण या शहरी या किसी भी क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। पहली नजर में लग सकता है कि इस तरह की सोच अपनी व्यापकता के कारण बहुत सी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकती है, पर इस समग्रता में इतनी रचनात्मकता है, और इसके उद्देश्य इतने खूबसूरत हैं कि इस राह पर चलने में कोई बोझ प्रतीत नहीं होगा अपितु साथ चलते हुए निरंतर प्रेरणादायक माहौल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सच मानें तो यही स्वदेशी का मूल भाव है।