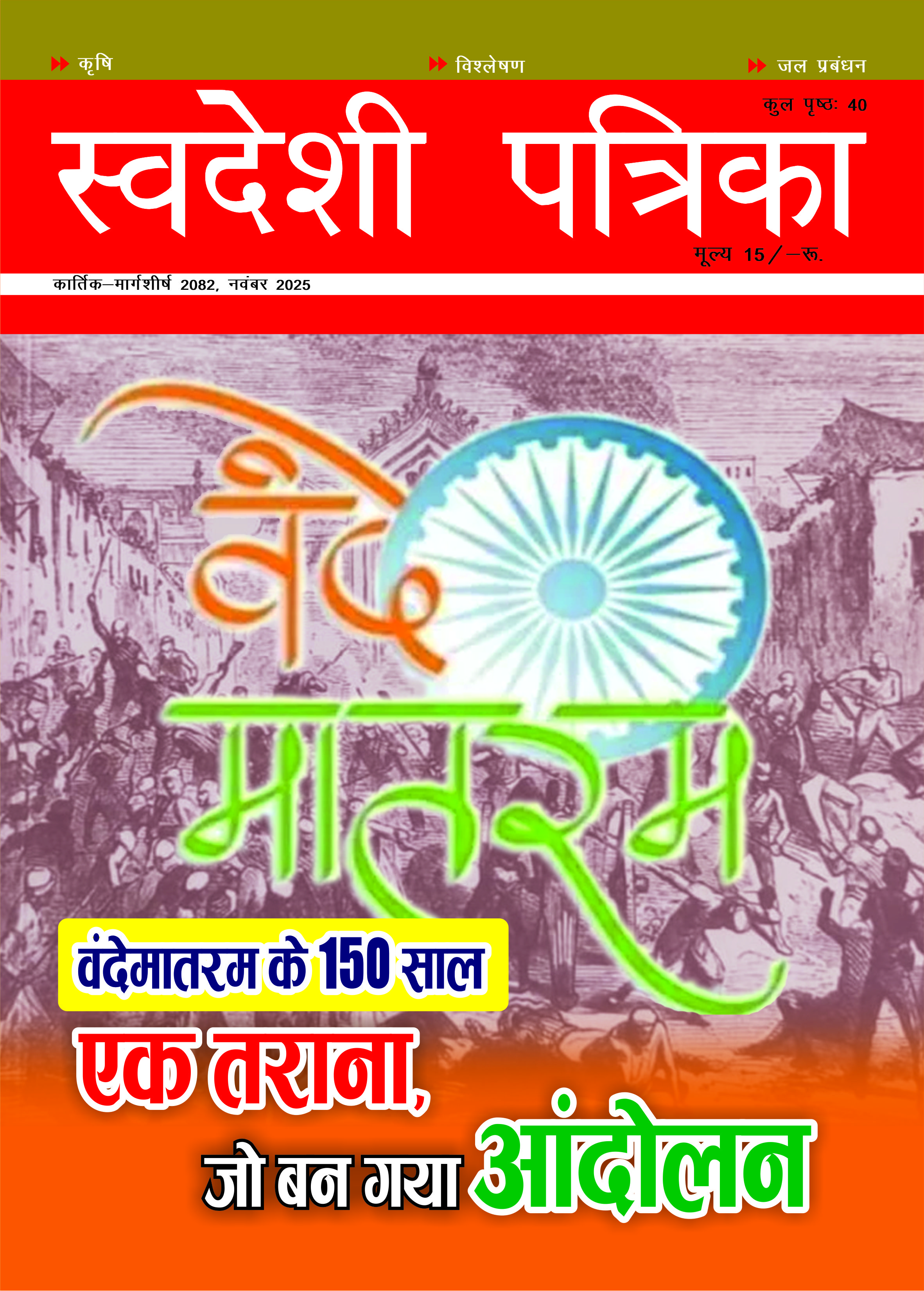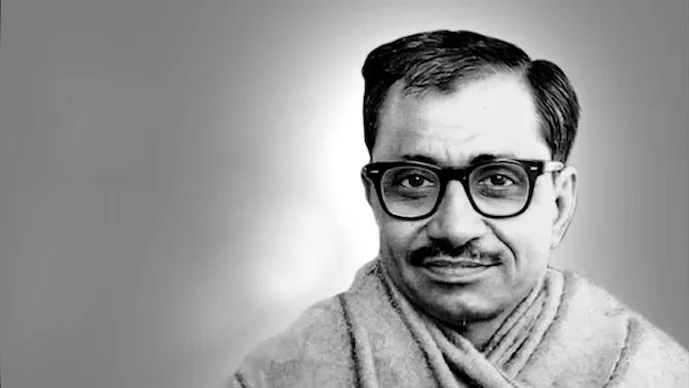
आज और भी प्रासंगिक हैं पं. दीनदयाल उपाध्याय
पिछले सौ वर्षों में दुनिया ने प्रौद्योगिकी, भौतिक वस्तुओं के उत्पादन और आर्थिक सेवाओं के विस्तार के मामले में अभूतपूर्व प्रगति की है। अगर हम इस प्रगति को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में मापें, तो हम पाते हैं कि पिछले सौ वर्षों में दुनिया की जीडीपी कई गुना बढ़ गई है। विभिन्न चरणों में हुई औद्योगिक क्रांतियों ने इस भौतिक विकास में योगदान दिया है। आम तौर पर लोग अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। बुनियादी ढाँचे, ऑटोमोबाइल, विमानन, अंतरिक्ष, संचार आदि के क्षेत्र में प्रगति सबसे उल्लेखनीय रही है। लेकिन साथ ही, पर्यावरण क्षरण, आर्थिक असमानताओं और सामाजिक विघटन के कारण मानवता ने अपने अस्तित्व के मूल आधार को ही संकट में डाल दिया है। हमारा समाज और व्यवस्था उस स्तर पर पहुँच गई है जहाँ हम देखते हैं कि अगर इन बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया तो मानव सभ्यता ही नहीं सृष्टि से जीवन ही विलुप्त हो सकता है। वर्तमान बुराइयों का मूल कारण यह है कि हमने यह मान लिया है कि यदि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, यदि अधिक ऊर्जा खपत होती है और जीडीपी बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि विकास हो रहा है। यह भी मान लिया गया कि इस भौतिक प्रगति से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस बढ़े हुए उत्पादन का लाभ स्वतः ही आम जनता तक पहुँचेगा और उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन हम ज़मीनी स्तर पर जो देखते हैं, कि असमानताएँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, जहाँ कुछ लोग विलासिता का आनंद ले रहे हैं और आम जनता गरीबी की चपेट में है। शायद, पर्यावरण के बिगड़ते हालात के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। हम देख रहे हैं कि दशकों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में निरंतर वृद्धि हो रही है, वैश्विक तापमान अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है, और लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के आसपास की बस्तियाँ खतरे में हैं, वायु की गुणवत्ता बदतर हो रही है जिससे साँस लेना भी मुश्किल हो रहा है, पानी और मिट्टी अभूतपूर्व रूप से प्रदूषित हो रहे हैं और इस प्रकार पृथ्वी रहने योग्य नहीं बच रही है। भौतिक प्रगति के साथ, मानवता को भौतिक प्रगति प्राप्त करने की लालसा और लालच के रूप में एक और झटका लगा, जिससे सामाजिक और पारिवारिक विघटन हुआ। मूल्यों में यह गिरावट व्यक्तिवाद के उदय के साथ और भी बढ़ गई।
आज, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि को विकास का एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है। लेकिन क्या जीडीपी सभी की भलाई और पर्यावरण संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है? शायद नहीं। युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि, वनों की कटाई, बीमारियों की बढ़ती घटनाओं आदि के साथ भी राष्ट्रों की जीडीपी बढ़ सकती है। इसलिए, हम जीडीपी में वृद्धि को अधिक खुशी का पैमाना नहीं मान सकते। यह और भी असंभव है कि जीडीपी में वृद्धि पिरामिड के निचले स्तर पर रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसके विपरीत, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकास का एक वैकल्पिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। वह दर्शन क्या है? उपाध्याय जी का दर्शन कहता है कि सच्चा विकास वह है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुख और सुविधा पहुँचाए, अर्थात अंत्योदय। आर्थिक विकास का लाभ तब तक अधूरा है जब तक वह समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक न पहुँचे। यही विचार आज के सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीतियों का भी मार्गदर्शन कर सकता है।
भारत की सांस्कृतिक परंपरा हमेशा से इस विचार पर आधारित रही है कि मनुष्य केवल एक आर्थिक इकाई नहीं है, बल्कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से युक्त एक समग्र इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। इसी गहन समझ के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन प्रस्तुत किया। यह दर्शन उस समय भी भारत की विकास यात्रा के लिए एक मार्गदर्शक था, और आज, जब वैश्विक आर्थिक असमानता, सामाजिक विखंडन और पर्यावरणीय संकट गहरा रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। आज की नीतियाँ मुख्यतः भौतिक प्रगति पर आधारित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी प्रगति में भी, लक्ष्य अक्सर “प्रतिस्पर्धात्मक लाभ“ और “आर्थिक लाभ“ माने जाते हैं। हालाँकि, मनुष्य केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं; उसके मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक आयाम भी हैं। यदि विकास शरीर और भौतिक संसाधनों तक सीमित है, तो समाज असंतुलित और तनावग्रस्त हो जाता है। उपाध्याय जी का दर्शन हमें याद दिलाता है कि विकास तभी वास्तविक है जब वह व्यक्ति के इन सभी पहलुओं का संतुलित तरीके से पोषित करे।
सामाजिक और आर्थिक असमानता भारत में लंबे समय से एक चुनौती रही है। जाति, धर्म और वर्ग के विभाजन आज भी समाज को विभाजित करने का प्रयास करते हैं। उपाध्याय समाज को एक “जीवित शरीर“ के रूप में देखते हैं, जहाँ प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, और कोई भी अंग दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं होता। यह दृष्टिकोण समाज में समानता ही नहीं, बल्कि समरसता भी स्थापित करता है, जहाँ सभी को समान सम्मान और महत्व प्राप्त होता है। आज के विखंडित समाज में यह विचार और भी आवश्यक हो गया है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट है। निरंतर औद्योगीकरण और उपभोक्तावाद ने प्रकृति के अत्यधिक दोहन को जन्म दिया है। ऐसे समय में, एकात्म मानव दर्शन हमें बताता है कि मनुष्य और प्रकृति शत्रु नहीं हैं, बल्कि एक सहजीवी संबंध में हैं। जब तक विकास पर्यावरण के अनुकूल और संतुलित नहीं होगा, तब तक वह सतत् नहीं हो सकता। यह दृष्टिकोण आधुनिक सतत् विकास से कहीं अधिक गहरा है क्योंकि यह न केवल संसाधन संरक्षण पर आधारित है, बल्कि प्रकृति को परिवार मानने की भारतीय संस्कृति पर भी आधारित है। वैश्वीकरण के दौर में, आर्थिक नीतियाँ बहुराष्ट्रीय निगमों और बाज़ार की ताकतों के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इससे सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता पर ख़तरा बढ़ गया है। एकात्म मानव दर्शन ’भारतीयता’, यानी भारतीयता की ओर लौटने का आह्वान करता है। यह कहता है कि नीतियाँ हमारी सांस्कृतिक चेतना और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। आज, यह दर्शन “आत्मनिर्भर भारत“ और “विकसित भारत“ जैसे राष्ट्रीय अभियानों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है।