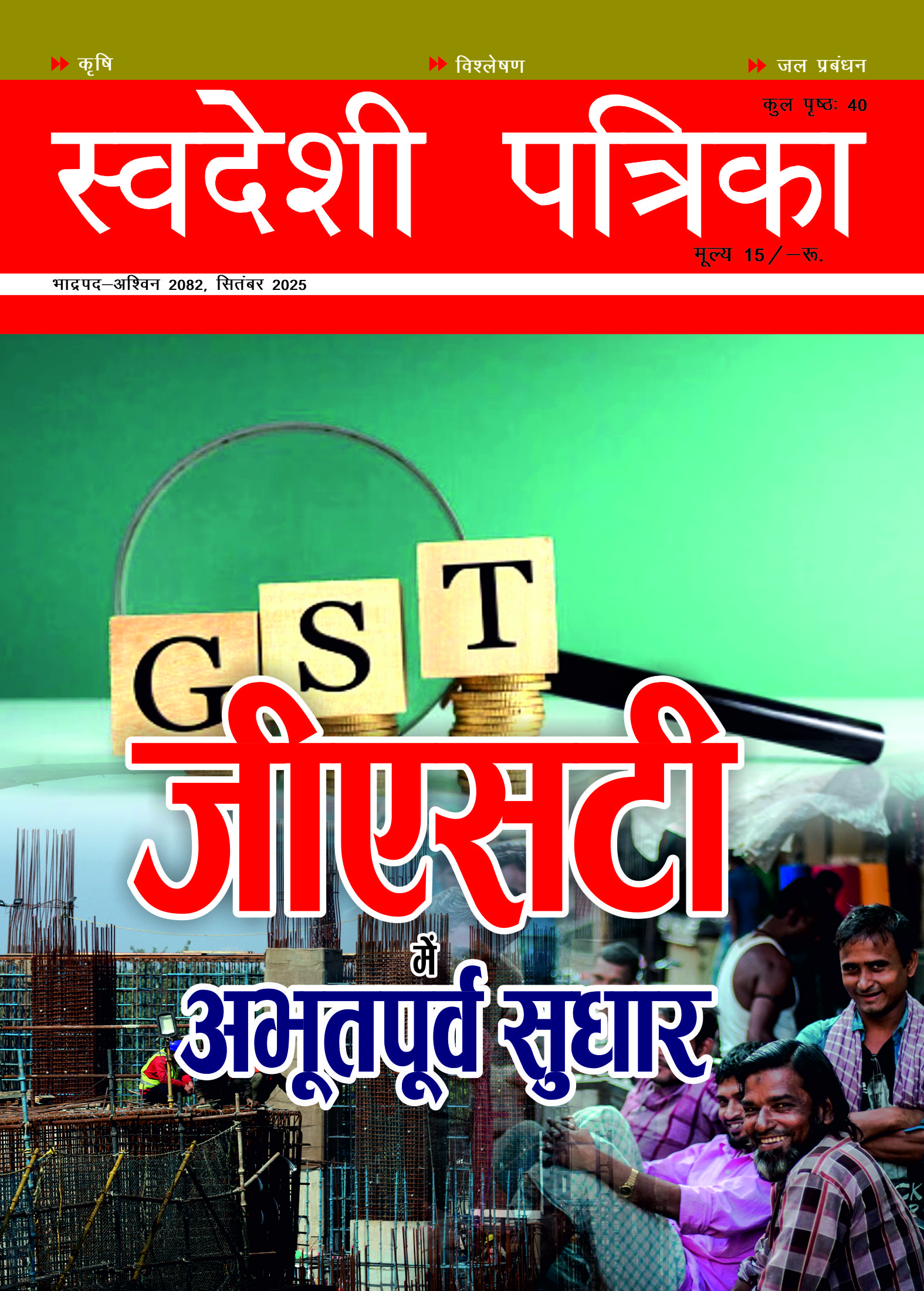भारत का विदेशी व्यापार और आत्मनिर्भरता
भारत को विदेशी व्यापार में ऐसी नीति अपनानी होगी जो एक ओर उच्च मूल्यवर्धित निर्यात से आर्थिक शक्ति बढ़ाए, और दूसरी ओर आवश्यक आयात को स्थायी एवं संतुलित ढंग से संचालित करे। इस प्रकार विदेशी व्यापार, आत्मनिर्भर भारत और मानव-केन्द्रित विकास की परिकल्पना का वास्तविक साधन बन सकता है। - अनिल जवलेकर
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने विदेशी व्यापार को नया आयाम दिया है। दूसरे महायुद्ध के बाद विदेशी व्यापार को एक मुक्त व्यापार की ओर जोर जबरदस्ती ले जाने वाला अमरिका अब संरक्षणात्मक व्यापार पर जोर दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सहूलियत वह दूसरे देशों को देने को तैयार नहीं है। यहाँ भी जोर-जबरदस्ती की बात हो रही है। भारत को तो धमकियां दर धमकियां मिल रही है। इसलिये वैश्विक व्यापार आज अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और अमेरिका तथा यूरोप के संरक्षणवाद से भारत जैसे विकासशील देश सकते में आ गये है। वैसे भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का हिस्सा बढ़ता जा रहा है और सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। भारत की अपनी संरचना विदेशी व्यापार में लचीलापन रखती है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, वैसे ही उसमें विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है। आयात तेज़ी में है और उसके मुकाबले निर्यात की गति अपेक्षाकृत कम है। और तो और विदेशी व्यापार में घाटा भी बढ रहा है, इन्हीं कारणों से आत्मनिर्भरता की ज़रूरत महसूस होती है।
विदेशी व्यापार संकल्पना
वैसे कोई व्यक्ति, समाज या देश पूर्णतः सक्षम नहीं होता। किसी न किसी बात पर उसे दूसरे की जरूरत रहती है। इसलिए यह बात चर्चा का विषय नहीं है कि विदेश व्यापार होना चाहिए या नहीं। विदेश व्यापार अर्थव्यवस्था का अंगभूत क्षेत्र होता है और वैसे ही उसे देखना और समझना चाहिए। जब तक दुनिया में अलग-अलग देश है और पर्यावरण की दृष्टि से भी उनकी अलग-अलग विशेषताएँ तथा क्षमता है, तब तक विदेशों से व्यवहार भी होता रहेगा और व्यापार भी, और वह एक दूसरे को लाभदायक भी है। अपनी-अपनी विशेषताओं से भरा वस्तु तथा सेवाओं का आदान-प्रदान होना मानव जाति के हित में ही है। सवाल यह है कि यह व्यवहार और व्यापार किन शर्तों के आधार पर होगा और इसमें होने वाले फायदे-नुकसान को कैसे सुलझाया जाएगा। जरूरी है कि इसमें सभी देशों की अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और किसी पर भी अंतरराष्ट्रीय दबाव में व्यापार की मजबूरी न हो। अपनी विशेष क्षमता का उपयोग कर एक दूसरे की ज़रूरते पूरी हो, यही व्यवहार व्यापार को सफल बनाएगा। विदेशी व्यापार स्थानीय जीवन को समृद्ध करे, यही हर देश की नीति होनी चाहिए। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद हमें स्मरण कराता है कि नीति केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि मनुष्य, समाज और संस्कृति के उत्थान का माध्यम होनी चाहिए। इस दृष्टि से विदेश व्यापार या आयात-निर्यात नीति केवल फायदे-नुकसान का उपकरण नहीं, बल्कि स्थानीय समाज को वैश्विक अवसर से जोड़ने का साधन है।
भारतीय विदेश व्यापार की स्थिति
भारत का विदेशी व्यापार इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है - प्राचीन काल में भारत मसाले, वस्त्र और धातु-शिल्प के निर्यात से विश्व का “कारख़ाना” माना जाता था और व्यापार अधिशेष अर्जित करता था। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने इसे कच्चे माल के निर्यातक और तैयार वस्तुओं के आयातक में बदल दिया, जिससे पारंपरिक उद्योग नष्ट हुए और व्यापार घाटा बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1991 तक भारत ने आत्मनिर्भरता और आयात-प्रतिस्थापन की नीति अपनाई, जहाँ निर्यात सीमित और आयात नियंत्रण में रहा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण और सेवा-क्षेत्र (विशेषकर आईटी) ने भारत के विदेशी व्यापार को नई दिशा दी। आज भारत ऊर्जा व सोने के आयात पर निर्भर होने के बावजूद विविधीकृत निर्यात (फार्मा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेवाएँ) के साथ वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में जगह बनाने का प्रयास कर रहा है, और 2030 तक निर्यात में महत्त्वपूर्ण वृद्धि का लक्ष्य रखता है।
आज भारत का विदेशी व्यापार लगभग यूएस $820 अरब निर्यात और यूएस $915 अरब आयात (वित्तीय वर्ष 2024-25) तक पहुँच चुका है, जिससे करीब यूएस $94 अरब का व्यापार घाटा बनता है। निर्यात में इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, इंजीनियरिंग, सेवाएँ और कृषि-उत्पाद प्रमुख हैं, जबकि आयात में पेट्रोलियम, सोना, मशीनरी व इलेक्ट्रॉनिक घटक मुख्य हैं। भारत का व्यापार धीरे-धीरे विविधीकृत हो रहा है, पर ऊर्जा और कच्चे माल पर आयात-निर्भरता अभी भी बड़ी चुनौती है। प्रमुख साझेदारों में चीन (15 प्रतिशत आयात), अमेरिका (भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य), यूएई (तेल व सोना), और रूस (ऊर्जा) शामिल हैं। इन देशों के साथ व्यापार का स्वरूप अलग-अलग है - जहाँ अमेरिका व यूरोप को उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद और सेवाएँ भेजे जाते हैं, वहीं चीन व रूस से भारत को बड़े पैमाने पर ऊर्जा, कच्चा माल और विनिर्माण सामग्री मिलती है। इस प्रकार भारत का विदेशी व्यापार अवसर और निर्भरता, दोनों का मिश्रण है।
भारतीय विदेशी व्यापार का लचीलापन और नीति की गुंजाईश
भारतीय विदेशी व्यापार में लचीलापन स्पष्ट रूप से दिखता है - जब वैश्विक मांग बढ़ती है तो भारतीय निर्यात, विशेषकर आईटी सेवाएँ, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग वस्तुएँ, तेजी से प्रतिसाद देते हैं; वहीं कच्चे तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे आयात मूल्य में थोड़े उतार-चढ़ाव भी भारत के आयात बिल को भारी रूप से प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ है कि भारत के निर्यात अपेक्षाकृत मांग-लचीले हैं, जबकि आयात, खासकर ऊर्जा, अधिक अनिवार्य और कम लचीले रहते हैं। इसलिए भारत को ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत और दीर्घकालीन आयात समझौतों पर जोर देना होगा। साथ ही, निर्यात की विविधता बढ़ाने, उच्च मूल्य-वर्धित उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से गहरे जुड़ाव के लिए पीएलआई योजनाएँ, आरओडीटीईपी और एफटीए समझौते महत्वपूर्ण औजार हैं। इससे भारत का विदेशी व्यापार अधिक संतुलित, टिकाऊ और वैश्विक झटकों के प्रति लचीला बनाया जा सकता है।
भारतीय विदेशी व्यापार और आत्मनिर्भरता नीति
भारतीय विदेशी व्यापार को यदि एकात्म मानववाद के दृष्टिकोण से देखें तो यह केवल आयात-निर्यात संतुलन या विदेशी मुद्रा अर्जन का विषय नहीं रह जाता, बल्कि मानव-केन्द्रित, समाज-हितैषी और संतुलित विकास का माध्यम बन जाता है। पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारानुसार आर्थिक नीति का उद्देश्य मात्र उत्पादन-वृद्धि नहीं बल्कि समान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता है। इस संदर्भ में विदेशी व्यापार का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वह देश की मूलभूत जरूरतों को पूरा करे, घरेलू उद्योग और कृषि को प्रोत्साहित करे तथा आयात-निर्भरता को न्यूनतम करे।
आज भारत का निर्यात विविधीकृत हो रहा है - सेवाएँ, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद वैश्विक बाजार में मजबूत स्थान बना रहे हैं, परंतु आयात, विशेषकर ऊर्जा और सोने पर अत्यधिक निर्भरता, हमारी आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाती है। एकात्म मानववाद का मार्गदर्शन बताता है कि व्यापार नीति को केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर आधारित न रखकर, “आवश्यकताओं की पूर्ति $ स्वदेशी उत्पादन क्षमता $ समाजोन्मुख संतुलन” पर केंद्रित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि भारत को विदेशी व्यापार में ऐसी नीति अपनानी होगी जो एक ओर उच्च मूल्यवर्धित निर्यात से आर्थिक शक्ति बढ़ाए, और दूसरी ओर आवश्यक आयात को स्थायी एवं संतुलित ढंग से संचालित करे। इस प्रकार विदेशी व्यापार, आत्मनिर्भर भारत और मानव-केन्द्रित विकास की परिकल्पना का वास्तविक साधन बन सकता है।